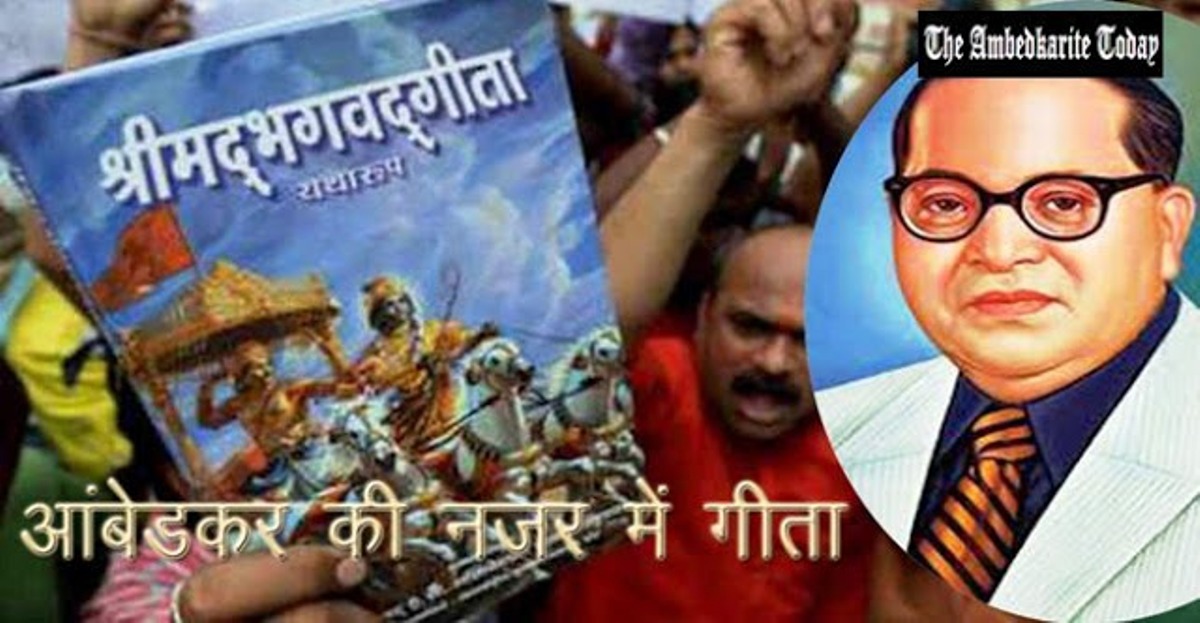प्राचीन भारत के साहित्य में भगवद्गीता का क्या स्थान है?
क्या यह हिंदू धर्म का उसी प्रकार का एक धर्मग्रंथ हैं, जिस प्रकार ईसाई धर्म की बाइबिल है। हिंदू इसे अपना धर्मग्रंथ मानते हैं। अगर यह धर्मग्रंथ है, तब यह वस्तुतः क्या शिक्षा देता है? यह किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? इस विषय पर जो विद्वान कुछ कहने के लिए सक्षम हैं, उन्होंने इस प्रश्न के जो उत्तर दिए हैं, वे एक-दूसरे से इतने भिन्न हैं कि सचमुच आश्चर्य होता है। बोटलिंग्क (रिचार्ड्स गार्बे द्वारा अपने इंट्रोडक्शन टू दि भगवद्गीता में उद्धृत {इंडियन एंटीक्वैरी 1918 परिशिष्टांक}) लिखते हैं:
राजा से न करे , क्योंकि वह अपनी ही शक्ति से उन सभी लोगों को दंडित कर सकता है, तो उसे क्षति पहुंचाते हैं।
11.32. उसकी निजी शक्ति, जो केवल उसी पर निर्भर करती है, राजकीय शक्ति से प्रबल होती है, जो कि दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर है। अतः ब्राह्मण अपनी शक्ति के द्वारा ही अपने शत्रुओं का दमन कर सकता है।
11.33 वह निस्संकोच शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग कर सकता है, जो अथर्वन को प्राप्त हुए और जो उसके द्वारा अंगिरस को दिए गए, क्योंकि वाणी ही ब्राह्मण का शस्त्रास्त्र है, जिससे वह अपने शत्रुओं का विनाश कर सकता है।
9.320. यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के विरुद्ध सभी अवसरों पर हिंसक ढंग से शस्त्र उठाता है तो उसे स्वयं वह ब्राह्मण दंड देगा, क्योंकि क्षत्रिय मूल रूप से ब्राह्मण से ही पैदा हुआ है।
ब्राह्मण जब तक शस्त्रास्त्र न ग्रहण करे, तब तक क्षत्रिय को किस प्रकार दंडित कर सकता है? मनु इसे जानता था, अतः वह क्षत्रियों को दंडित करने के लिए ब्राह्मणों को शस्त्रास्त्र ग्रहण करने का अधिकार देता है।
12.100. वेदज्ञाता मनुष्य सेनापतित्व, राज्य दंडप्रणेतृत्व (न्यायाधीश आदि होने) और संपूर्ण लोकों के स्वामित्व के योग्य है।
मनु चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का इतना प्रबल पक्षधर है कि उसने यह मौलिक परिवर्तन करने में कोई कमी नहीं रखी। ब्राह्मण द्वारा शस्त्रास्त्र ग्रहण करने का आग्रह एक मौलिक परिवर्तन है, जो मनु पूर्व विद्यमान नहीं था। ब्राह्मण द्वारा शस्त्रास्त्र ग्रहण न किए जाने का बड़ा कठोर नियम था। मनु पूर्व आपस्तंब धर्म सूत्र में यह नियम निम्नानुसार वर्णित है:
1. 10.29.6. ब्राह्मण अपने हाथ में, चाहे उसे जांचने की ही इच्छा क्यों न हो, शस्त्र ग्रहण नहीं करेगा।
2. 24.18. गौर की रक्षा हेतु ब्राह्मण अथवा वर्ण के विषय में भ्रांति होने पर ब्राह्मण और वैश्य भी शस्त्रास्त्र ग्रहण कर सकते हैं, जो धर्म-सम्मत और हर कीमत पर मान्य है।
गीता में उच्च और सुंदर भाव तो हैं, लेकिन इसके साथ कुछ दुर्बल पक्ष भी हैं, परस्पर विरोधी उक्तियां (टीकाकारों ने जिन्हें क्षम्य समझा है और जिन्हें टीका करते समय छोड़ देने की कोशिश की है), जगह-जगह पुनरावृत्तियां, अतिशयोक्तियां, असंगतियां और नीरस उक्तियां।
होपकिंस (रिलिजन ऑफ इंडिया, पृ. 390-400) भगवद्गीता को उसकी महत्त्वपूर्णता और महत्त्वहीनता, तर्कपूर्णता और तर्कहीनता के कारण हिंदू साहित्य की एक विलक्षण कृति मानते हैं, आदिम दार्शनिक सिद्धांतों का अटपटा समुच्चय।
वह अपना मत व्यक्त करते हुए लिखते हैं:
हालांकि इस दैवी गीत में यत्र-तत्र ऊर्जा और संगीत की भव्यता है, तो भी वर्तमान काव्यकृति के रूप में यह एक अशक्त रचना है। एक ही बात को बार-बार कहा गया है। शब्दावली में और अर्थ में परस्पर विरोध के अनगिनत उदाहरण हैं, जितने कि पुनरावृत्तियों के। ये इतने अधिक हैं कि हर किसी को तब आश्चर्य होता है, जब इस कृति के बारे में यह कहा जाता है कि यह अद्भुत गीत है, जो रोमांच पैदा कर देता है।
होट्जमैन (गार्बे द्वारा उद्द्धृत) कहते हैं
“यह (भगवद्गीता) सर्वेश्वरवादी कविता का वैष्णव संस्करण है।
गार्बे (इंट्रोडक्शन टू भगवद्गीता) लिखते हैं
इस कविता की समग्र प्रकृति विन्यास और रचना की दृष्टि से मुख्यतः आस्तिक है। कृष्ण के नाम के एक इष्ट देवता मानवीय रूप से उपस्थित हो अपने मत की व्याख्या करते हैं और अपने श्रोता को यह आदेश देते हैं कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के साथ-साथ सर्वप्रथम उनमें भक्ति रखे और अपने-आपको समर्पित कर दे और इस देवता के साथ-साथ, जिसे यथासंभव इष्ट रूप से व्यक्त किया गया है और सारी कविता में प्रमुख है, सर्वोच्च सिद्धांत के रूप में अक्सर निर्वेयक्तिक तटस्थ ब्रह्म की सत्ता भी, जो परम है, स्पष्ट प्रतीत होती है। कृष्ण कभी यह कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, जिसने समस्त विश्व और प्राणियों की सृष्टि की है और जो सबका नियामक है, कभी वह ब्रह्म और माया (भ्रम वेदांत की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि मानव प्राणी का चरम लक्ष्य इस सांसरिक भ्रम से मुक्ति पाना और ब्रह्म रूप हो जाना है। ये दोनों सिद्धांत-ईश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद एक-दूसरे में मिला दिए गए हैं, एक-दूसरे का अनुगमन करते हैं, एक दूसरे से सर्वथा पृथक हो जाते हैं और कभी ये पूरी तरह अपृथक और कभी थोड़ा-बहुत पृथक रहते हैं। ऐसा भी नहीं हैं कि किसी एक को निम्न या बाह्य दिखाया गया हो और दूसरे को उच्च या गुप्त सिद्धांत। यह भी कहीं नहीं बताया गया है कि सत्य के ज्ञान के लिए ईश्वरवाद आरंभिक उपाय है या यह उसका प्रतीक है और वेदांत का सर्वेश्वरवाद स्वतः (चरम) सत्य है, लेकिन ये दोनों विचारधाराएं लगभग पूरे पाठ में इस प्रकार दिखाई गई हैं कि वस्तुतः इनमें कोई भेद नहीं है, न तो शाब्दिक और न तत्वतः।
श्री तेलंग (भगवद्गीता (एस.ई.बी.) इंट्रोडक्शन, पृ. 22) का कहना है
“गीता में कई ऐसे स्थल हैं जिनका एक-दूसरे के साथ मेल बिठाना कठिन है और इनमें संगत बिठाने की कोई कोशिश भी नहीं की गई है। उदाहरणार्थ, अध्याय 7 के श्लोक 16 में कृष्ण अपने भक्तों को चार श्रेणियों में विभाजित करते हैं, इनमें से एक श्रेणी उनकी है, जो ‘ज्ञानी’ हैं, जिनके बारे में कृष्ण कहते हैं कि वह उन्हें ‘अपना ही रूप’ मानते हैं। इस परम पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति के बारे में कुछ कहने के लिए इससे अधिक उपयुक्त शब्दावली शायद ही मिल सकती थी और अध्याय 6 के श्लोक 46 में हमें यह पढ़ने को मिलता है कि भक्त न केवल तपस्वी से, बल्कि ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। भाष्यकार इस श्लोक में ‘ज्ञानी’ शब्द की इस प्रकार व्याख्या कर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं कि ये वे व्यक्ति हैं, जिन्होंने शास्त्रों और उनके सामर्थ्य में ज्ञान प्राप्त कर लिया है। यह कोई ऐसी टिप्पणी नहीं है, जिस पर विचार करना आवश्यक है। वहां शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा गया है और इन परिस्थितियों में मैं इसे स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूं। दूसरी ओर अध्याय 4 के श्लोक 39 से यह व्यक्त होता है कि भक्ति की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठतम है – यह एक उच्चतर अवस्था है, जहां भक्ति के द्वारा पहुंचा जा सकता है, भक्ति एक सोपान है। गीता में अध्याय 12 के श्लोक 12 में ध्यान को ज्ञान की तुलना में वरीयता दी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी संगति भी अध्याय 7 के श्लोक 16 के साथ नहीं बैठती। एक और उदाहरण लीजिए। गीता में अध्याय 4 के श्लोक 14 में कहा गया है कि ईश्वर (कृष्ण) किसी के पाप या पुण्य का भागी नहीं है, लेकिन अध्याय 9 के श्लोक 24 में कृष्ण अपने को सभी यज्ञों का ‘भोक्ता और प्रभु’ बताते हैं। तब यह प्रश्न उठता है कि परमात्मा उसका भोग कैसे कर सकता है, जो उसे प्राप्त नहीं होता।
अध्याय 9 के श्लोक 29 में पुनः कृष्ण घोषणा करते हैं कि मेरे लिए न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है, लेकिन अध्याय 12 का अंतिम श्लोक तो इसके ठीक विपरीत है। इस अध्याय में अनेक श्लोक एक साथ मिलते हैं, जिनमें कृष्ण भावपूर्ण रीति से कहते दिखाए गए हैं कि ऐसा-ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। उसी प्रकार उन श्लोकों में, जहां कृष्ण अपने अध्यात्म का सार प्रस्तुत करते हैं, वह अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझे प्रिय हो। कृष्ण यह भी कहते हैं कि उन्हें वह भक्त प्रिय है, जो गीता के रहस्य को परब्रह्म के संदर्भ में उद्घाटित करता है। (अध्याय 7 के श्लोक 17 को भी देखिए, जहां कृष्ण को ज्ञानवान व्यक्ति प्रिय बताया गया है।) ‘हम इस उद्धरण का कि कृष्ण को न कोई प्रिय है, न अप्रिय, अध्याय 16 के श्लोक 18 और बाद के श्लोकों में कृष्ण की ही उक्तियों के साथ किस प्रकार मेल बिठा सकते हैं? वहां राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वह उनके प्रति किसी प्रिय भाव का द्योतक नहीं है, जब कृष्ण कहते है, मैं ऐसे लोगों को असुर योनि में फेंक देता हूं, जहां से वे कष्टों और निकृष्टतम गति में जा गिरते हैं।’ ऐसे व्यक्तियों का वर्णन उन्हें’ न अप्रिय, न प्रिय’ कहकर करना शायद ही उचित हो। मुझे ऐसा लगता है कि गीता में ये असंगतियां वास्तविक असंगतियां हैं और ऐसी नहीं हैं कि जिनकी व्याख्या न की जा सके, बल्कि मेरा विचार है कि और जैसा कि प्रो. मैक्समूलर कहते हैं, यह ऐसी मनःस्थिति को दिखाती है, जहां व्यक्ति सत्य के बारे में अनुमान मात्र लगा रहा होता है, न कि उस मनःस्थिति को, जहां एक पूर्ण और सुगठित दर्शन-सिद्धांत की व्याख्या की जा रही होती है। इस बात का तनिक भी संकेत नहीं हैं कि लेखक को इन असंगतियों की जानकारी है। जैसा कि विभिन्न उद्धरणों से पता चलता है और मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, किसी प्रसंग-विशेष पर विचार करते समय कुछ अर्द्धसत्यों को, जो स्पष्टत एक-दूसरे से मेल नहीं खाते, एक जगह सुव्यवस्थित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। अगर ऐसा किया गया होता, तब ये सारी की सारी असंगतियां विलीन हो गई होतीं।‘
यह विचार उनक विचारकों के हैं, जिन्हें आधुनिक कहा जा सकता है। अगर हम पुराने रूढ़ीवादी पंडितों के विचारों को पढ़ें, तब हमें भिन्न-भिन्न मत मिलेंगे। एक मत यह है कि भगवद्गीता किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, और इसमें मोक्ष प्राप्ति के तीनों मार्गों का समान रूप से निवर्चन किया गया है। ये मार्ग हैं- (1) कर्ममार्ग, (2) भक्ति मार्ग और (3) ज्ञान मार्ग। यह ग्रंथ मोक्ष प्राप्ति के तीनों मार्गों की उपयोगिता का उपदेश देता है। ये पंडितगण अपने इस मत की पुष्टि में कि गीता में सभी मार्गों की उपयोगिता को स्वीकार किया गया है, यह कहते हैं कि इस ग्रंथ के 18 अध्यायों में से अध्याय 1 से 6 तक ज्ञान मार्ग, अध्याय 7 से 12 तक कर्म मार्ग और अध्याय 12 से 18 तक भक्ति मार्ग का उपदेश मिलता है। इनकी यह धारणा है कि गीता मोक्ष प्राप्ति के तीनों ही मार्गों को उचित बताती है।
इन पंडितों के दृष्टिकोण शंकराचार्य और श्री तिलक का है। दोनों ही विद्वानों को परंपरावादी लेखकों कर श्रेणी में रखा जा सकता है। शंकराचार्य का दृष्टिकोण यह था कि भगवद्गीता में ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया गया है और ज्ञान मार्ग ही मोक्ष का एक मात्र सही मार्ग है। श्री तिलक (देखिए, गीता रहस्य (दूसरा संस्कारण), खंड 2, अध्याय 14, स्फुट) अन्य विद्वानों में से किसी विद्वान के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। वे इस दृष्टिकोण का खंडन करते हैं कि गीता में अनेक विसंगतियां हैं। वे उन पंडितों से भी सहमत नहीं हैं, जो कहते हैं कि भगवद्गीता मोक्ष के तीन मार्गों को उचित मानती है। शंकराचार्य के समान उनका अभिमत है कि भगवद्गीता निश्चिय सिद्धांत के बारे में उपदेश देती है, परंतु उनका मत शंकराचार्य से भिन्न है और उनकी धारणा है कि गीता में कर्म योग का नहीं, बल्कि ज्ञान योग का उपदेश किया है।
गीता में जो कुछ कहा गया है, उसके बारे में इतने भिन्न-भिन्न मतों का होना केवल आश्चर्य की बात नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति यह पूछ सकता है कि विद्वानों में इतना मतभेद क्यों है? इस प्रश्न के उत्तर में मेरा निवेदन है कि विद्वानों ने ऐसे लक्ष्य की खोज की है, जो मिथ्या है। वे इस अनुमान पर भगवद्गीता के संदेश की खोज करते हैं कि कुरान, बाइबिल अथवा धम्मपद के समान गीता भी किसी धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। मेरे मतानुसार यह अनुमान ही मिथ्या है। भगवद्गीता कोई ईश्वरीय वाणी नहीं है, इसलिए उसमें कोई संदेश नहीं है और इसमें किसी संदेश की खोज करना व्यर्थ है। निस्संदेह यह प्रश्न पूछा जा सकता है : यदि भगवद्गीता कोई ईश्वरीय वाणी नहीं है, तो फिर यह क्या है? मेरा उत्तर है कि भगवद्गीता न तो धर्म ग्रंथ है और नही यह दर्शन का ग्रंथ है। भगवद्गीता ने दार्शनिक आधार पर धर्म के कतिपय सिद्धांतों की पुष्टि की है। यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर भगवद्गीता को धर्मग्रंथ अथवा दर्शन का ग्रंथ कहता है, तो वह अपने मुंह मियां मिट्ठू बन सकता है, परंतु यह वस्तुतः दोनों में से एक भी नहीं है। इस ग्रंथ में दर्शन का प्रयोग धर्म की पुष्टि के लिए किया गया है। मेरे प्रतिद्वंद्वी केवल राय बताने से ही संतुष्ट नही होंगे। वे इस बात पर बल देंगे कि मैं अपनी स्थापना को विशिष्टतथ्यों का संदर्भ देकर सिद्ध करूँ। यह कोई कठिन बात नहीं है। वास्तव में यह सबसे सरल कार्य है।
भगवद्गीता का अध्ययन करने पर सबसे पहली बात जो हमें मिलती है, वह यह कि इसमें युद्ध को संगत ठहराया गया है। स्वयं अर्जुन ने युद्ध तथा संपत्ति के लिए लोगों की हत्या करने का विरोध किया। कृष्ण ने युद्ध तथा युद्ध में हत्याओं की दार्शनिक आधार पर पुष्टि की। युद्ध की यह दार्शनिक पुष्टि भगवद्गीता के अध्याय 2 के श्लोक 2 से 28 तक दी गई है। युद्ध की दार्शनिक पुष्टि तर्क की दो कसौटियों पर आधारित है। पहला तर्क यह है कि संसार नश्वर है तथा मनुष्य मृत्युधर्मी है। वस्तुओं का अंत होना निश्चित है। मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। जो बुद्धिमान हैं, उनके लिए इस बात से क्या अंतर पड़ेगा कि मनुष्य की स्वाभाविक मृत्यु होती है अथवा वह हिंसा के फलस्वरूप मृत्यु को प्राप्त करता हैं? जीवन अस्वाभाविक है, इस बात पर आंसू क्यों बहाए जाएं कि उसका अंत हो गया है? मृत्यु अनिवार्य है, फिर इस बात पर क्यों विचार किया जाए कि मृत्यु किस प्रकार हुई? दूसरा तर्क प्रस्तुत करते हुए युद्ध की आवश्यकता को सिद्ध किया गया है और यह सोचना भ्रम है कि शरीर और आत्मा एक हैं। वे अलग-अलग हैं। वे केवल स्पष्ट रूप से अलग-अलग ही नहीं, परंतु वे दोनों अलग-अलग इसलिए हैं कि शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अमर और अविनाशी है। जब मृत्यु होती है तो शरीर का अंत हो जाता है। आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता और आत्मा कभी भी नहीं मरती, यहां तक कि वायु इसे सुखा नहीं सकती, अग्नि इसे जला नहीं सकती और हथियार इसे काट नहीं सकते। इसलिए यह कहना भूल है कि जब व्यक्ति मर जाता है, तो उसकी आत्मा भी मर जाती है। वास्तव में स्थिति यह है कि शरीर मर जाता है। उसकी आत्मा मृत शरीर को उसी प्रकार त्याग देती है, जैसे व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, वह नए वस्त्र धारण करता है तथा अपना जीवन बिताता है। चूंकि आत्मा कभी भी नहीं मरती है, अतः व्यक्ति की हत्या होने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए युद्ध और हत्या-जनित पश्चाताप अथवा संकोच, यही भगवद्गीता का तर्क है।
एक अन्य सिद्धांत, जिसे भगवद्गीता में प्रस्तुत किया गया है, वह चातुर्वर्ण्य की दार्शनिक पुष्टि है। निस्संदेह भगवद्गीता में बताया गया कि चातुर्वर्ण्य ईश्वर का सृजन है और इसलिए यह अति पवित्र है, परंतु गीता में यह इस कारण वैध नहीं बताया गया है। इसके लिए दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया गया है तथा उसे मनुष्य के स्वाभाविक और जन्मजात गुणों के साथ जोड़ दिया गया है। भगवद्गीता में कहा गया है कि पुरुष के वर्ण का निर्धारण मनमाने ढंग से नहीं हुआ है, परंतु उसका निर्धारण मनुष्य के स्वाभाविक और जन्मजात गुणों (भगवद्गीता, 4,13) के आधार पर किया जाता है।
भगवद्गीता में तीसरा सिद्धांत कर्म योग की दार्शनिक पृष्ठभूमि बताकर प्रस्तुत किया गया है। भगवद्गीता के अनुसार कर्म मार्ग का अर्थ है मोक्ष के लिए यज्ञ आदि संपन्न करना। भगवद्गीता में कर्म योग का प्रतिपादन किया गया है और इस हेतु उन बातों का निराकरण किया गया है, जो अनावश्यक रूप से कर्मयोग में पैदा हो गई हैं, जिन्होंने उसे ढक दिया है और विकृत कर दिया है। पहली बात है अंधविश्वास। गीता का उद्देश्य कर्म योग की आवश्यक शर्त के रूप में बुद्धि योग (भगवद्गीता, 4,13., 2, 39-53) के सिद्धांत का निरूपण कर उस अंधविश्वास को समाप्त करना है। यदि व्यक्ति स्थितप्रज्ञ, अर्थात् संयत बुद्धि हो जाए तो कर्मकांड करना कोई गलत बात नहीं है। दूसरा दोष यह है कि कर्मकांड के पीछे स्वार्थ निहित था और यही स्वार्थ कर्म-संपादन के लिए प्रेरणा रहा। इस दोष के निराकरण के लिए भगवद्गीता में अनासक्ति अर्थात् कर्म के फल की इच्छा किए बिना कर्म (भगवद्गीता, 2,47) के संपादन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। गीता में कर्म मार्ग (यह भगवद्गीता, 2,48 में निष्कर्ष के रूप में मिलता है) की पुष्टि यह तर्क प्रस्तुत करके की गई है कि अगर इसके मूल में बुद्धि योग हो और कर्म के कारण किसी फल क इच्छा की भावना न हो, तो कर्मकांड के सिद्धांत में कोई त्रुटि नहीं है। इसी क्रम में अन्य सिद्धांतों के संबंध में विचार करना उचित ही है कि गीता में दार्शनिक आधार पर इनकी पुष्टि किस प्रकार की गई है, जो पहले अस्तित्व में ही नहीं थे, परंतु यह तभी हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति भगवद्गीता पर कोई शोध प्रबंध लिखे। यह इस अध्याय के कार्य-क्षेत्र के परे की बात है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन भारतीय साहित्य में गीता के समुचित महत्त्व का आकलन करना है। इसलिए मैंने मुख्य-मुख्य सिद्धांतों को चुना है, ताकि मैं अपनी व्याख्या की पुष्टि कर सकूं। निश्चित ही मेरी व्याख्या को लेकर दो और प्रश्न हो सकते हैं। भगवद्गीता में जिन सिद्धांतों की दार्शनिक पुष्टि की गई है, वे किन व्यक्तियों के हैं? भगवद्गीता के लिए इन सिद्धांतों की पुष्टि करना क्यों आवश्यक हो गया था?
प्रथम प्रश्न से प्रारंभ किया जाए। गीता मे जिन सिद्धांतों की पुष्टि की गई है, वे प्रतिक्रांति के सिद्धांत हैं, जो प्रतिक्रांति की बाइबिल अर्थात् जैमिनि कृत पूर्वमीमांसा में वर्णित हैं। इस तर्क को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कठिनाई है, तो मुख्यतः कर्म योग शब्द का गलत अर्थ करने से संबंधित है। भगवद्गीता के अधिकांश भाष्यकार ‘कर्म योग’ शब्द का अनुवाद ‘कार्य’ और ‘ज्ञान योग’ शब्द का अनुवाद ‘ज्ञान’ करते हैं और भगवद्गीता पर यह समझकर विचार करते हैं कि इसमें सामान्य रूप में ज्ञान और कर्म में तुलना और उनके अंतर का विवेचन किया गया है। यह बिलकुल गलत है। भगवद्गीता का उद्देश्य कर्म बनाम ज्ञान का विषय पर कोई सामान्य या दार्शनिक चर्चा करना नहीं है। वास्तव में गीता का संबंध विशेष विषय से है, सामान्य विषय से नहीं है। कर्मयोग अथवा कर्म के बारे में गीता का आशय उन सिद्धांतों से है, जो जैमिनि के कर्मकांड में दिए गए हैं और ज्ञान योग अथवा ज्ञान का आशय उन सिद्धांतों से है, जो बादरायण के ब्रह्म सूत्र में दिए गए हैं। गीता में कर्म की चर्चा का आशय कर्म या अकर्म, निवृत्तिवाद या प्रवृत्तिवाद से नहीं है, सामान्य अर्थ में इस चर्चा का आशय धार्मिक, अनुष्ठान तथा उनके पालन से है और जिसने भी गीता को पढ़ा है, वह इस बात से इंकार नहीं करेगा। गीता को एक ऐसे दल की प्रचार सामग्री (पेंफलेट) के स्तर से ऊंचा उठाकर लिखने का प्रयास किया गया, जो क्षुद्र विवाद में उलझ गया था और जिससे ऐसा लगे कि यह उच्च दर्शन के विषयों पर लिखा गया कोई अच्छा-खासा भाष्य हो।
इसलिए कर्म और ज्ञान शब्दों के अर्थ का विस्तार किया गया और इन्हें सामान्य शब्दों के रूप में ग्रहीत किया गया। देशभक्त भारतीयों के इस रहस्य के लिए मुख्य दोष श्री तिलक को दिया जाना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ है कि इन गलत अर्थों ने लोगों को भ्रम में डाल दिया और वे यह विश्वास करने लगे कि भगवद्गीता एक स्वतंत्र स्वतः पूर्ण ग्रंथ है तथा इसका उस साहित्य से कोई संबंध नहीं है, जो इस ग्रंथ से पूर्व था, परंतु यदि कोई व्यक्ति कर्म योग शब्द के अर्थ को वैसा ही ग्रहण करना चाहता है, जैसा कि भगवद्गीता में दिया गया है, तो वह व्यक्ति इस बात से सहमत हो जाएगा कि भगवद्गीता में कर्म योग के बारे में कोई अन्य बात नहीं कही गई है, परंतु वहां आशय कर्मकांड के उन सिद्धांतों से है, जिनका प्रतिपादन जैमिनी द्वारा किया गया था तथा जिन्हें गीता द्वारा पुनर्जीवित और पुष्ट करने का प्रयास किया गया है।
अब दूसरे प्रश्न पर विचार किया जाए। भगवद्गीता में प्रतिक्रांति के सिद्धांतों की पुष्टि करना क्यों आवश्यक समझा गया? मैं सोचता हूं कि इसका उत्तर सरल है। यह इसलिए किया गया, जिससे इन सिद्धांतों की बौद्ध धर्म के जबरदस्त प्रभाव से रक्षा की जा सके और यही कारण है कि भगवद्गीता की रचना की गई। बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने अहिंसा का उपदेश ही नहीं दिया, अपितु ब्राह्मणों को छोड़कर अधिकांश लोगों ने अहिंसा को जीवन-शैली के रूप में स्वीकार भी कर लिया था। उनके मन में हिंसा के प्रति घृणा पैदा हो चुकी थी। बुद्ध ने चातुर्वर्ण्य के विरुद्ध उपदेश दिए। उन्होंने चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत का खंडन करने के लिए बड़ी कटु उपमाएं दीं। चातुर्वर्ण्य का ढांचा चरमरा गया। चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था उलट-पुलट थी। शूद्र और महिलाएं संन्यासी हो सकते थे, ये ऐसी प्रतिष्ठा थी, जिससे प्रतिक्रांति ने उन्हें वंचित कर दिया। बुद्ध ने कर्मकांड और यज्ञ कर्म की भर्त्सना की। उन्होंने इस आधार पर भी उनकी भर्त्सना की कि इन कर्मों के पीछे अपनी स्वार्थ-सिद्धि की भावना छिपी हुई थी। इस आक्रमण के विरुद्ध प्रतिक्रांतिवादियों का क्या उत्तर था? केवल यही कि ये बातें वेदों के आदेश हैं, वेद भ्रमातीत हैं, अतः इन सिद्धांतों के बारे में शंका नहीं की जानी चाहिए।
बौद्ध-काल में, जो भारत का सबसे अधिक प्रबुद्ध और तर्कसम्मत युग था, ऐसे सिद्धांतों के लिए कोई स्थान नहीं था, जो अविवेक, दुराग्रह, तर्कहीन और अस्थिर धारणाओं पर आश्रित हों। जो लोग अहिंसा पर उसे एक जीवन-शैली मानकर विश्वास करने लगे थे और जो उसे जीवन में नियम के रूप में अपना चुके थे, उनसे इस सिद्धांत को स्वीकार करने की आशा किस प्रकार की जा सकती थी कि हत्या करने पर क्षत्रिय को पाप इसलिए नहीं लग सकता, क्योंकि वेदों में ऐसा करना उसका कर्तव्य बताया गया है। जिन लोगों ने सामाजिक एकता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था तथा जो व्यक्ति के गुणों के आधार पर समाज का पुनर्निर्माण कर रहे थे, वे श्रेणीबद्ध करने वाले चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत और केवल जन्म के आधार पर व्यक्तियों के वर्गीकरण को क्यों स्वीकार करते, क्योंकि वेदों ने ऐसा कहा है? जिन लोगों ने बुद्ध के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था कि समाज में सभी दुःख तृष्णा के कारण हैं, अथवा जिसे संग्रह की प्रवृत्ति कहा जाता है, वे उस धर्म को क्यों स्वीकार करते, जो लोगों को यज्ञादि कर्म (बलि) से लाभ प्राप्ति के लिए इसलिए प्रेरित करता है कि ऐसा करना वेद-सम्मत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बौद्ध धर्म के तेजी से बढ़ते प्रभाव से जैमिनी के प्रतिक्रांति सिद्धांत डगमगा उठे थे और वे चकनाचूर हो जाते, यदि उन्हें भगवद्गीता द्वारा दिए गए प्रतिक्रांतिवादी सिद्धांतों की दार्शनिक पुष्टि किसी भी प्रकार से अकाट्य नहीं हैं। भगवद्गीता द्वारा इस बात की दार्शनिक आधार पर पुष्टि करना कि क्षत्रिय का कर्तव्य हत्या करना है, एक बचकानी बात है। यह कहना कि हत्या करना हत्या नहीं है, क्योंकि जिसकी हत्या की जाती है, वह शरीर की है और वह आत्मा की नहीं है, यह हत्या-कर्म एक ऐसा बचाव है, जिसे कभी भी नहीं सुना गया है। यदि कृष्ण को अपने उस मुवक्किल की ओर से अधिवक्ता के रूप में उपस्थित होना पड़ता, जिस पर हत्या का मुकदमा चलाया जा रहा है और वे भगवद्गीता में बताए गए सिद्धांत को उस अपराधी के बचाव के लिए प्रस्तुत करते, तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं हैं कि उन्हें पागलखाने में भेज दिया जाता।
इसी प्रकार भगवद्गीता में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के सिद्धांत की पुष्टि करना भी बचकाना कार्य है। कृष्ण इस सिद्धांत की पुष्टि सांख्य के गुण सिद्धांत के आधार पर करते हैं, परंतु कृष्ण को अपनी त्रुटि का अनुभव नहीं होता। चातुर्वर्ण्य में चार वर्ण होते हैं, परंतु सांख्य के अनुसार गुणों की संख्या तीन है। चार वर्णों की व्यवस्था को उस दर्शन पर किस प्रकार आधारित किया जा सकता है, जिसमें तीन से अधिक वर्णों को मान्यता ही नहीं दी गई है? भगवद्गीता में प्रतिक्रिया के सिद्धांतों की दार्शनिक आधार पर पुष्टि करने के लिए जो यह सारा प्रयास किया गया है, वह बहुत ही बचकाना है और इसके बारे में एक क्षण भी गंभीर रूप में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इसमें संदेह नहीं है कि भगवद्गीता की सहायता के बिना प्रतिक्रांति अपने सिद्धांतों की निस्सारता के कारण कभी की समाप्त हो गई होती। भगवद्गीता की यह भूमिका क्रांतिकारियों को चाहे जितनी भी शरारतपूर्ण लगे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवद्गीता ने प्रतिक्रांति को पुनर्जीवन प्रदान किया और यदि प्रतिक्रांति आज भी जीवित है तो यह उस दार्शनिक पुष्टि के आडंबर के कारण है, जो इसे भगवद्गीता से प्राप्त हुई है, यह सब कुछ वेद-विरुद्ध और यज्ञ-विरुद्ध है। जैसा कि भगवद्गीता के अन्य अंशों से यह बात विदित होगी कि वेदों और शास्त्रों (16.23-24: 17.11-13.24) के प्राधिकार के विरुद्ध नहीं है। यह यज्ञ (3.9-15) की अनिवार्यता के विरुद्ध नहीं हैं। यह दोनों के महत्त्व को पुष्ट करती है। इस प्रकार जैमिनी की पूर्व-मीमांसा और भगवद्गीता में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। यदि कुछ विशेरुा बात है तो यह कि भगवद्गीता अधिक दृढ़ता से प्रतिक्रांति का समर्थन करती है, जबकि जैमिनी कृत पूर्व-मीमांसा ने इतना समर्थन नहीं किया है। यह विशिष्ट इसलिए है कि यह प्रतिक्रांति को दार्शनिक सिद्धांत देती है और इसलिए उसका आधार स्थायी है, जैसा कि पहले कभी नहीं था और उसके बिना प्रतिक्रांति का अस्तित्व बना रहना भी संभव नहीं था।
जैमिनी की पूर्व-मीमांसा की तुलना में भगवद्गीता की दार्शनिक पुष्टि अधिक विशिष्ट है और भगवद्गीता का यह दार्शनिक समर्थन है, जो प्रतिक्रांति के केंद्रीय सिद्धांत अर्थात् चातुर्वर्ण्य को प्रदान करती है। चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत की पुष्टि तथा व्यवहार में उसका अनुपालन ही भगवद्गीता की मूल भावना प्रतीत होती है। कृष्ण यह कहकर संतुष्ट नहीं होते कि चातुर्वर्ण्य गुण-कर्म पर आधारित है और वह इससे भी आगे बढ़ जाते हैं और दो आदेश देते हैं। पहला आदेश अध्याय 3, श्लोक 26 में दिया गया है।
कृष्ण कहते हैं: ज्ञानी व्यक्ति को प्रतिवाद कर अज्ञानी व्यक्ति के मन में संदेह उत्पन्न नहीं करना चाहिए, जो कर्मकांड का अनुसरण करता हो, जिसमें निश्चय ही चातुर्वर्ण्य के नियम भी सम्मिलित हैं अर्थात् हमें लोगों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए कि कहीं वे कर्मकांड के सिद्धांत और उसमें शामिल अन्य बातों के विरोध में न उठ खड़े हों। दूसरा आदेश भगवद्गीता के अध्याय 18, श्लोक 41-48 में दिया गया है। इसमें कृष्ण ने कहा है कि प्रत्येक को अपने वर्ण के लिए निर्धारित कर्तव्य करना चाहिए और उन्हें अन्य कोई कर्तव्य नहीं करना चाहिए तथा वह उन लोगों को चेतावनी देते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं तथा उनके भक्त हैं कि ये लोग केवल भक्ति करने से ही मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेंगे, बल्कि इसके लिए उन्हें भक्ति के साथ उन कर्तव्यों को भी करना होगा, जो उनके वर्ण के लिए निर्धारित हैं। संक्षेप में, शूद्र चाहे कितना ही महान भक्त क्यों न हो, यदि उसने शूद्र के कर्तव्य का उल्लंघन किया है। अर्थात् उसने उच्च वर्गों के लोगों की सेवा में जीवनयापन नहीं किया है, तो उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मेरी दूसरी स्थापना यह है कि भगवद्गीता का मुख्य आशय जैमिनी को नया समर्थन देना था और इसके कम से कम वे अंश, जो जैमिनी के सिद्धांतों की दार्शनिक आधार पर पुष्टि करते हैं, वे जैमिनी की पूर्व-मीमांसा के बाद और जब जैमिनी के सिद्धांत कार्यान्वित हो चुके थे, तब लिखे गए थे। मेरी तीसरी स्थापना यह है कि बौद्ध धर्म के क्रांतिकारी और तार्किक विचारों के प्रहार के फलस्वरूप भगवद्गीता के द्वारा प्रतिक्रांति के सिद्धांतों की दार्शनिक आधार पर पुष्टि की जानी आवश्यक हो गई थी।
अब मैं उन आपत्तियों को लेता हूं, जो मेरी स्थापनाओं की वैधता के संबंध में उठाई जा सकती हैं। मुझसे कहा जा सकता है कि जो मैं यह कहता हूं कि भगवद्गीता का प्रणयन-काल बौद्ध धर्म और जैमिनी की पूर्व मीमांसा के बाद का है, वह केवल अनुमान है ओर इस अनुमान के पीछे कोई प्रमाण नहीं है। मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि मेरी स्थापना अधिकांश भारतीय विद्वानों के द्वारा स्वीकृत दृष्टिकोण के विपरीत है, जिसका आग्रह यह स्वीकार करने में हैं कि भगवद्गीता की रचना अतिप्राचीन-काल की है और यह बौद्ध धर्म तथा जैमिनी से पूर्ववर्ती है, न कि इस बात की खोज करने में है कि भगवद्गीता का संदेश क्या है और मानव-जीवन के मार्गदर्शक के रूप में उसका क्या मूल्य है। यह बात विशेषकर श्री तेलंग व श्री तिलक के बारे में खरी उतरती है, परंतु जैसा कि गार्बे (इंट्रोडक्शन (इंडियन एंटीक्वैरी परिशिष्टांक) भूमिका, पृ. 30) ने लिखा है,
तेलंग के लिए जैसा कि प्रत्येक हिंदू के संबंध में है, जो चाहे कितना ही प्रबुद्ध क्यों न हो, भगवद्गीता को अति प्राचीन समझना, आस्था की बात है और जहां यह भावना प्रबल हो, वहां आलोचना हो ही नहीं सकती
प्रोफेसर गार्बे कहते हैं
गीता के प्रणयन काल को निश्चित करने का कार्य प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, जिसने इस समस्या को हल करने का निष्ठापूर्वक प्रयत्न किया है, एक बहुत ही कठिन कार्य कहा गया है और यह कठिनाई (हर तरह से) तब और भी बढ़ जाती है, जब इस समस्या को दुहरे रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात् मूल गीता के प्रणयन-काल के साथ-साथ उसके संशोधन करने के समय को भी निश्चित करना। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस मामले में प्रायः हम किसी निश्चित निर्णय पर न पहुंच कर केवल संभावनाओं पर पहुंच सकेंगे।
ये संभावनाएं क्या हैं, मुझे कोई संदेह नहीं कि ये संभावनाएं मेरे शोध प्रबंध के पक्ष में हैं। वास्तव में, मैं जितना विचार कर सकता हूं, उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं है। इस प्रश्न की जांच करने में सर्वप्रथम गीता से ही सीधा साक्ष्य प्रस्तुत करता हूं, जिसमें यह बताया गया है कि गीता का प्रणयन जैमिनी की पूर्वमीमांसा और बौद्ध धर्म के बाद हुआ।
भगवद्गीता का अध्याय 3, श्लोक 9-13 का विशेष महत्त्व है। इस संबंध में यह सत्य है कि भगवद्गीता में जैमिनी नाम का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है, ना मीमांसा का नाम ही दिया गया है, परंतु क्या कोई इसमें संदेह है कि भगवद्गीता के अध्याय 3, श्लोक 9-18 में उन सिद्धांतों का वर्णन है, जो जैमिनी की पूर्व मीमांसा में दिए गए हैं? यहां तक कि श्री तिलक (गीता रहस्य, खंड 2, 916-922) भी, जो भगवद्गीता की प्राचीनता में विश्वास करते हैं, यह स्वीकार करते हैं कि भगवद्गीता, पूर्व-मीमांसा के सिद्धांतों का परीक्षण करती है। इस तर्क को प्रस्तुत करने का एक अन्य तरीका है। जैमिनी ने शुद्ध और सरल कर्म योग का उपदेश दिया है। दूसरी ओर भगवद्गीता ने अनासक्ति कर्म का उपदेश दिया है। इस प्रकार गीता एक ऐसे सिद्धांत का उपदेश देती है, जिसे आमूल संशोधित कर दिया गया है। भगवद्गीता कर्म योग में संशोधन ही नहीं करती, अपितु कुछ कठोर शब्दों (भगवद्गीता, 2,42-46 और 18.66) में शुद्ध और सरल कर्म योग के समर्थकों की आलोचना करती है। यदि गीता जैमिनी से पूर्व का ग्रंथ है, तो पाठक जैमिनी से आशा करेगा कि यह भगवद्गीता की आलोचना करते और समुचित उत्तर देते, परंतु हमें भगवद्गीता के इस अनासक्ति कर्म योग के संबंध में जैमिनी में कोई संदर्भ नहीं मिलता। ऐसा क्यों हैं? इसका सही उत्तर है कि संशोधन जैमिनी के बाद किया गया ओर उनसे पहले नहीं किया गया था, यह सरलतापूर्वक सिद्ध कर देता है कि भगवद्गीता की रचना जैमिनी की पूर्व-मीमांसा के बाद की गई।
हालांकि भगवद्गीता में पूर्व मीमांसा का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें बादरायण के ब्रह्म सूत्र (भगवद्गीता, 13.4) का भी नाम से उल्लेख किया गया है। ब्रह्मसूत्र का यह संदर्भ अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रत्यक्षतः यह निष्कर्ष निकलता है कि गीता की रचना ब्रह्मसूत्र के बाद की गई है।
श्री तिलक (गीता रहस्य, 2.749) यह स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म सूत्रों का यह जो उल्लेख किया गया है, उसका आश्य स्पष्ट और निश्चित रूप से उसी ग्रंथ से है, जो अब हमें उपलब्ध है। यह उल्लेखनीय है कि तेलंग (भगवद्गीता, (एस.बी.ई.) इंट्रोडक्शन, पृ. 31) ने इस विषय की सरसरी चर्चा की है और बताया कि भगवद्गीता में जिस ब्रह्मसूत्र का उल्लेख किया गया है, वह वर्तमान ग्रंथ से भिन्न है। वह इस इतने महत्त्वपूर्ण वक्तव्य की पुष्टि के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते, पर वह श्री वेबर (हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर, पृ. 242) के अनुमान के आधार पर दिए गए वक्तव्य पर विश्वास करते हैं – जो उनके ‘ट्रीटाइज इन इंडियन लिटरेचर’ नामक ग्रंथ की पाद-टिप्पणी में उल्लेखित है और बिना किसी साक्ष्य, जिसमें यह कहा गया है कि भगवद्गीता में ब्रह्म सूत्र का उल्लेख नाम की अपेक्षा जातिवाचक है। श्री तेलंग के इस मत का कारण कोई विशेष उद्देश्य रहा होग, ऐसा कहना उचित नहीं हैं, परंतु यह कहना अनुचित नहीं हैं कि श्री तेलंग (दूसरी ओर यह भी कहा जा सकता है कि तेलंग ने शीघ्र ही इस संदर्भ को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनका यह मत था कि ब्रह्मसूत्र प्राचीन ग्रंथ है। देखिए गीता रहस्य, खंड 2) ने ब्रह्मसूत्र के इस संदर्भ को जिस रूप में स्वीकार किया है, वह वेबर पर आश्रित है, जो इस विंटरनिट्ज के मत को स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मसूत्र की रचना 500 ईसवी में हुई थी। अगर वह और गहराई में गए होते, तब उनके अभीष्ट मत का खंडन हो गया होता। भगवद्गीता की प्राचीनता का इस प्रकार इस निष्कर्ष की पुष्टि के लिए हमारे पास प्रचुर आंतरिक साक्ष्य है कि गीता का प्रणयन जैमिनी की पूर्व-मीमांसा और बादरायण के ब्रह्मसूत्र के बाद हुआ।
क्या भगवद्गीता बौद्ध मत के पूर्व की रचना है? यह प्रश्न श्री तेलंग द्वारा उठाया गया था। अब हम दूसरी बात पर आते हैं। शाक्य मुनि के महान सुधारो के संबंध में गीता की स्थिति क्या है? यह प्रश्न विशेषकर बौद्ध सिद्धांतों और गीता के सिद्धांतों में उल्लेखनीय समानता के संदर्भ में बहुत ही रोचक है, जिसके बारे में हमने अपने अनुवाद की पाद-टिप्पणियों में ध्यान आकृष्ट किया है, लेकिन इस प्रश्न को हल करने के लिए दुर्भाग्य से अपेक्षित तथ्य नहीं मिलते। यह अवश्य है कि प्रो. विल्सन का विचार है कि गीता (एसेज आन संस्कृत लिटरेचर, खंड 3, पृ. 150) में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के चिह्न मिलते हैं, लेकिन उनकी यह धारणा बौद्धों और चार्वाकों या भौतिकवादियों के बीच पाए जाने वाले मतभेद पर आश्रित थी (इस बारे में इंट्रोडक्टरी एसेज टू अवर गीता इन वर्स, पृ.11 पर क्रमशः हमारा मत देखें।)। इस संदर्भ के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। गीता में बौद्ध धर्म का उल्लेख नहीं है, यह एक ‘नकारात्मक तर्क’ है और अपर्याप्त है। यह तर्क मेरे विचार से, संतोषजनक भी नहीं है, हालांकि जैसा कि मैंने अन्यत्र कहा है (इंट्रोडक्शन टू गीता इन इंग्लिश वर्स, पृ. 5 क्रमशः) ‘गीता में जो कुछ कहा गया है, उनमें से कुछ बातें बौद्ध धर्म के समनुरूप हैं। हालांकि गीता में उसके पूर्ववर्ती विचारकों के चिह्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मिलते हैं, लेकिन इस प्रश्न के तथ्यों के बारे में एक दृष्टिकोण ऐसा है, जो मेरे विचार में उस निष्कर्ष की पुष्टि करता है, जिस पर उक्त नकारात्मक तर्क के द्वारा पहुंचा जा सकता है। बुद्ध जिन तथ्यों के कारण ब्राह्मण धर्म का विरोध करते हैं, वह वेदों के वास्तविक अधिकार और वर्णों में अंतर के बारे में सही दृष्टिकोण को लेकर है। सैद्धांतिक चिंतन के अनेक क्षेत्रों में बौद्ध धर्म अब भी पुराने ब्राह्मणवाद का एक रूप है (मैक्समूलर के हिब्बर्ट लैक्चर्स, पृ. 137, वेबर्स इंडियन लिटरेचर, पृ. 288-89, राइस डेविड्स का बुद्ध धर्म का उत्कृष्ट लघु ग्रंथ, पृ. 151 और डेविड की पुस्तक का पृ. 83 भी देखें)। यह विभिन्न समनुरूपताओं के आधार पर, जिनकी ओर हमने ध्यान आकृष्ट किया है, स्पष्ट हो जाता है। अब इन दोनों आधारों पर गीता स्वतः उन विचारों के प्रति प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करती है, जो उसके रचना-काल के समय विद्यमान था। बौद्ध धर्म की तरह गीता वेदों को पूर्णतः अस्वीकृत नहीं करती, बल्कि उन्हें एक ओर टिका देती है। गीता वर्ण-व्यवस्था का उन्मूलन नहीं करती। यह वर्णव्यवस्था को कुछ कम निराधार बताती है। इसलिए इन दोनों अनुमानों में से एक अनुमान इन तथ्यों के आधार पर युक्तियुक्त लगता है। या तो गीता और बौद्ध धर्म दोनों एक ही समनुरूप आध्यात्मिक क्रांति की अभिव्यक्ति हैं, जिसने उस समय के धर्म के ढांचे को हिला दिया था, इसमें गीता आरंभ की स्थिति या इस क्रांति का आरंभिक रूप थी या बौद्ध धर्म ब्राह्मणवाद पर हावी होने लगा था और गीता उसे पुष्ट करने का प्रयास थी अर्थात् गीता में उन पक्षों पर ध्यान दिया गया, जो निर्बल थे, निर्बलतर पक्ष पहले ही त्यागे जा चुके थे। मैं बाद वाली स्थिति को स्वीकार नहीं करता। इसका कारण यह है कि हालांकि गीता का रचनाकार वेदों की सत्ता को चुनौती देता है, तो भी गीता में प्राचीन हिंदू व्यवस्था पर सशक्त प्रहार के प्रति कोई समर्थन के संकेत नहीं मिलते। इसके अलावा यह बात भी है कि ऐसा करते समय वह वही करता है, जो उसके पहले किया गया, या जो उसके समकालिक कर रहे थे। ये तथ्य उक्त नकारात्मक तर्क के निष्कर्ष को पुष्ट करते हैं। मेरे विचार में बौद्ध धर्म उच्च आध्यात्मिक विषयों पर वैसी ही अभिव्यक्ति है, जैसी कि हमें उपनिषद और गीता में मिलती है। (तुलना कीजिए वेबर की हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर, पृ. 285। श्री डेविड की पुस्तक बुद्धिज्म में पृ. 94 पर हमें प्रामाणिक बौद्ध कृति से संदर्भ मिलता है, जिसमें आत्मा का वर्णन मिलता है। इसकी तुलना गीता में दिए गए तद्विषयक सिद्धांत से करिए। हम देखते हैं कि दोनों इंद्रियों आदि के साथ आत्मा के तादाम्य को अस्वीकृत करते हैं। गीता आत्मा को इनसे भिन्न स्वीकार करती है। बौद्ध धर्म इसे भी अस्वीकृत करता है और इंद्रियों के अतिरिक्त किसी सत्ता को नहीं मानता)
मैंने इस उद्धरण को पूरा-पूरा इसलिए उद्धृत किया है कि ऐसा ही सभी हिंदू विद्वानों का मत है। उनमें से कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि भगवद्गीता किसी भी रूप में बौद्ध धर्म से प्रभावित है। ये विद्वान इसे अस्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि गीता ने बौद्ध धर्म से कुछ ग्रहण किया है। यही दृष्टिकोण प्रो. राधाकृष्णन का और श्री तिलक का भी है। जब कभी भगवद्गीता और बौद्ध धर्म में बहुत अधिक विचारों के साम्य होने की बात उठती है, तब उसे अस्वीकार कर दिया जाता है और यह तर्क दिया जाता है कि यह उपनिषदों से ग्रहण किया गया है। यह प्रतिक्रांतिकारियों की ठेठ निम्न कोटि की वृत्ति है कि ये बौद्ध धर्म को कोई भी श्रेय नहीं प्रदान करना चाहते।
इस मनोवृत्ति से उन सभी को भारी दुःख पहुंचता है, जिन्होंने भगवद्गीता और बौद्ध सुत्तों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, क्योंकि यदि इस कथन में कोई सत्यता है कि गीता में सांख्य दर्शन भरा हुआ है, तो इस कथन में उससे भी अधिक सत्यता है कि गीता बौद्ध विचारों से भरी हुई है (इस विषय पर कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश श्री एस.डी. बुद्धिराजा, एम.ए., एल.एल. बी. की भगवद्गीता की तुलना कीजिए। लेखक ने गीता और बौद्ध धर्म की पाठ्यमूलक समानता की ओर ध्यान आकृष्ट करने की बार-बार कोशिश की है)। यह समानता केवल विचारों में ही नहीं, बल्कि भाषा में भी है। यह कुछेक उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा कि यह कहां तक सच है।
भगवद्गीता में ब्रह-निर्वाण (मैक्समूलर, महापरिनिब्बान सुत्त, पृ. 63) पर विवेचन किया गया है। कोई व्यक्ति ब्रह्म-निर्वाण तक किन साधनों से होकर पहुंच सकता है, वे भगवद्गीता में इस प्रकार बताए गए हैं : (1) श्रद्धा (अपने में विश्वास), (2) व्यवसाय (दृढ़ निश्चय), (3) स्मृति (लक्ष्य का स्मरण), (4) समाधि (मन लगाकर चिंतन) और (5) प्रज्ञा (अंतदृष्टि या यथातथ्य ज्ञान) गीता ने निर्वाण सिद्धांत कहां से लिया? निश्चय ही यह सिद्धांत उपनिषदों से नहीं लिया गया है, क्योकि किसी भी उपनिषद में निर्वाण शब्द का उल्लेख नहीं है। यह संपूर्ण विचारधारा बौद्धों की है और यह बौद्ध धर्म से ली गई है। यदि इस संबंध में किसी को संदेह है तो उसे भगवद्गीता के ब्रह्म-निर्वाण की तुलना बौद्ध धर्म की निर्वाण संबंधी अवधारणा से करनी चाहिए कि जिसका विवेचन महापरिनिब्बान सुत्त में किया गया है। हम देखेंगे कि ये दोनों एक हैं, जिसे गीता में ब्रह्म-निर्वाण की अपेक्षा ब्रह्म-निर्वाण की संपूर्ण अवधारणा कहीं से ग्रहण की है और ऐसा यह विचार बौद्ध धर्म से लिए गए इस तथ्य को छिपाने के लिए किया गया है?
एक अन्य उदाहरण लीजिए। अध्याय 7 के श्लोक 13-20 में इस बात का विवेचन किया गया है कि कृष्ण को कौन प्रिय है, वह व्यक्ति जो ज्ञानी है, वह व्यक्ति जो कर्म करता है अथवा वह व्यक्ति जो भक्त है। कृष्ण कहते हैं कि उनको भक्त प्रिय है, परंतु वह यह भी कहते हैं कि उसमें भक्ति के शुद्ध गुण होने चाहिए। सच्चे भक्त के क्या गुण होते हैं? कृष्ण के अनुसार, सच्चा भक्त वही है, जो (1) मैत्री (निश्छल सहानुभूति), (2) करूणा (दया), (3) मुदित (सहानुभूतिपूर्ण आनंद) और (4) उपेक्षा (अंतबंधता) का आचरण करता है। भगवद्गीता में सच्चे भक्त के ये लक्षण कहां से लिए गए हैं? यहां भी इसका स्रोत बौद्ध धर्म ही है। यदि कोई व्यक्ति प्रमाण चाहता है तो वह मापदान सुत्त (देखिए, महापदान सुत्त) और तेविज्जा सुत्त (देखिए, तेविज्जा सुत्त) से इसकी तुलना करे, जहां बुद्ध उन भावनाओं (मानसिक प्रवृत्तियों) का उपदेश देते हैं, जो हृदय को संयमित करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। इस तुलना से यह सिद्ध हो जाएगा कि यह संपूर्ण विचारधारा बौद्ध धर्म से ली गई है और यह शब्दशः अंगीकार की गई है।
तीसरा उदाहरण लीजिए। अध्याय 13 में भगवद्गीता में क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विषय का विवेचन किया गया है। भगवद्गीता के श्लोक 7-11 में कृष्ण ने यह बताया है कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, जो इस प्रकार है –
दंभरहितता (दीनता), निरहंकार,अहिंसा अथवा अहानिकारक, क्षमा, आर्जव (स्पष्टता), गुरु भक्ति, शुचिता, दृढ़ता, आत्म-संयम, इंद्रिय संबंध विषयों में अनिच्छा, अहं का प्रभाव, जन्म,मृत्यु, जरा और व्याधि से संबंधित दुःख और पाप पर विचार, ममत्व का अभाव, पुत्र, पत्नी, घर, शरीर तथा अन्य से अनासक्ति, प्रिय और अप्रिय दोनों स्थितियों में समभाव, मुझमें एकाग्र चिंतन सहित अनन्य भक्ति, पृथक स्थान का सेवन (एकांत में मनन, ध्यान), सांसारिक मनुष्यों की समाज के प्रति विरक्ति, आत्म से संबंधित ज्ञान का निरंतर मनन, तत्व (सांख्य दर्शन) के सही आशय का बोध या अनुभव, यह सब ज्ञान कहलाता है, इससे विपरीत जो कुछ भी है, वह अज्ञान है।
जिस किसी को बुद्ध के सिद्धांतों की थोड़ी बहुत भी जानकारी है, क्या वह यह इंकार कर सकता है कि भगवद्गीता के इन श्लोकों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की शब्दशः पुनरोक्ति नहीं की गई है?
भगवद्गीता में अध्याय 13 के श्लोक 5,6,18,19 में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत कर्म की नवीन प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है, जैसे (1) यज्ञ (बलि), (2) दान (उपहार), (3) तप (प्रायश्चित), (4) भोजन और (5) स्वाध्याय (वैदिक अध्ययन)। प्राचीन विचारों की इस नवीन व्याख्या का स्रोत क्या है? इसकी तुलना उससे की जाए जो मज्झिम निकाय 286,16 में बुद्ध के द्वारा कहा गया है? क्या कोई इसमें संदेह कर सकता है कि कृष्ण ने अध्याय 17 के श्लोक 5,6,18,19 में बुद्ध के शब्दों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं किया है?
मैंने सैद्धांतिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण उद्धरण चुने हैं, ये उनके कुछेक उदाहरण हैं। जो लोग इस विषय के अध्ययन करने में रुचि रखते हैं, वे गीता और बौद्ध धर्म के बीच समानताओं के उन संदर्भों को देख सकते हैं, जो श्री तेलंग ने भगवद्गीता के अपने संस्करण की पाद-टिप्पणियों में दिए हैं तथा अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं, परंतु मैंने जो उदाहरण दिए हैं, वह यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि भगवद्गीता में बौद्ध धर्म की विचारधारा का कितना अधिक समावेश है और भगवद्गीता ने बौद्ध धर्म से कितना अधिक ग्रहण किया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भगवद्गीता की रचना सोद्देश्य रूप में बौद्ध धर्म के सुत्तों (सूत्रों) के आधार पर की गई है। इसमें जो कथोपकथन हैं, वह बुद्ध के सुत्त (सूत्र) हैं। बौद्ध धर्म ने महिलाओं और शूद्रों को उद्धार का आश्वासन दिया है। बौद्ध धर्मावलंबियों का कहना हे,
मैं बुद्ध धर्म और संघ की शरण में जाता हूं। ठीक इसी प्रकार कृष्ण कहते हैं, धर्मों को त्याग दो और स्वयं को मुझे समर्पित कर दो।
जितनी समानता बौद्ध धर्म और भगवद्गीता में मिलती है, उतनी अन्यत्र कहीं नहीं मिलती।
मैंने यह बताया कि गीता पूर्व-मीमांसा के बाद की और बौद्ध धर्म के भी बाद की रचना है। मैं अपनी स्थापना को समाप्त कर सकता था, परंतु मैा अनुभव करता हूं कि यह संभव नहीं हैं, क्योंकि मेरी स्थापना के विरुद्ध एक तर्क शेष है, जिसका उत्तर दिया जाना आवश्यक है। यह भी तिलक का तर्क है। यह एक बुद्धिकौशल है। श्री तिलक यह अनुभव करते हैं कि भगवद्गीता और बौद्ध धर्म, दोनों में विचारों और उनकी अभिव्यक्ति में अनेक समानताएं हैं। चूंकि बौद्ध धर्म भगवद्गीता से प्राचीन है, अतः यह स्वाभाविक है कि भगवद्गीता की स्थिति ऋणी की है और बौद्ध धर्म की ऋणदाता की है। यह सीधी सी बात श्री तिलक को रुचिकर नहीं है और उन सभी लोगों को भी नहीं सुहाती, जो प्रतिक्रांति को उचित मानते हैं। उन सभी के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि प्रतिक्रांति को क्रांति का ऋणी नहीं होना चाहिए। इस कठिनाई को दूर करने के लिए श्री तिलक ने एक नयी बात खोज निकाली। उन्होंने हीनयान बौद्धधर्म और महायान बौद्धधर्म के बीच अंतर बताया है तथा यह कहा कि महायान बौद्ध धर्म भगवद्गीता के बाद अस्तित्व में आया और यदि बौद्ध धर्म तथा भगवद्गीता के बीच कोई समानताएं हैं तो भगवद्गीता से महायान बौद्ध धर्मावलंबियों के द्वारा विचार ग्रहण किए जाने के कारण हैं। इससे दो प्रश्न उठते हैं। महायान बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की क्या तिथि है? भगवद्गीता की रचना की तिथि क्या है? श्री तिलक का तर्क एक बुद्धिकौशल और चतुराई है, परंतु इसमें कोई सार नहीं है। पहले तो यह मौलिक नहीं है। यह विंटरनिट्ज (हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर (अंग्रेजी अनुवाद), खंड 2, पृ. 229, पाद टिप्पणी) और केर्न (मैनुअल आफ इंडियन बुद्धिज्म, पृ. 122, पाद टिप्पणी) द्वारा सरसरी तौर पर की गई कतिपय टिप्पणियों के आधार पर है। ये टिप्पणियां उनकी पाद-टिप्पणियों में मिलती हैं। इनमें कहा गया है कि भगवद्गीता और महायान बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं हैं और यह समानताएं भगवद्गीता से ग्रहण किए गए विचारों के आधार पर हैं। इन टिप्पणियों की पुष्टि में विंटरनिट्ज, केर्न अथवा श्री तिलक द्वारा किसी विशेष अनुसंधान का साक्ष्य नहीं दिया गया है। ये सभी टिप्पणियां इन अनुमानों के आधार पर हैं कि भगवद्गीता महायान बौद्ध धर्म से पूर्व की रचना है।
इसके बाद मेरे सामने प्रश्न भगवद्गीता के रचना-काल का है और भगवद्गीता की तिथि के प्रश्न पर विचार करना है, और इस प्रश्न का विशेषकर उस मत के संदर्भ में विचार किया जाना है, जो श्री तिलक ने प्रस्तुत किया है। श्री तिलक (गीता रहस्य, खंड 2, पृ. 791-800) का मत है कि गीता, महाभारत का एक भाग है और इन दोनों का रचयिता व्यास नामक एक ही लेखक है, जिसने इन दोनों की रचना की थी। इसलिए गीता का रचना-काल वही होना चाहिए, जो महाभारत का रचना-काल है। श्री तिलक का यह तर्क है कि महाभारत शक संवत् से कम से कम 500 वर्ष पूर्व रचा गया, जिसका आधार यह है कि महाभारत की कथाएं मेगस्थनीज को पता थीं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक राजदूत के रूप में लगभग 300 वर्ष ईसा पूर्व में भारत आए थे। शक संवत् 78 ईसवी में प्रारंभ हुआ। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवद्गीता की रचना 422 ईसा पूर्व में की गई थी। वर्तमान गीता के रचना-काल के बारे में यही उनका मत है। उनके मतानुसार मूल गीता, महाभारत की अपेक्षा कुछ शताब्दियां पुरानी होनी चाहिए। यदि भगवद्गीता में दी गई परंपरा पर विश्वास किया जाए कि भगवद्गीता में धर्म की शिक्षा प्राचीन-काल में नर द्वारा नारायण को दी गई थी, तो ऐसी स्थिति में महाभारत की रचना की तिथि के बारे में श्री तिलक का मत तर्कसंगत नहीं है। पहली बात तो यह है कि यहां का अनुमान किया गया है कि संपूर्ण भगवद्गीता और संपूर्ण महाभारत की रचना एक ही बार, एक ही समय और एक ही व्यक्ति द्वारा की गई। परंपरा और इन दोनों ग्रंथों में प्राप्त अंतः साक्ष्य की दृष्टि से इस अनुमान का कोई औचित्य नहीं है। अगर हम महाभारत तक अपने विचार-विमर्श को सीमित रखें, तो पता चलेगा कि श्री तिलक द्वारा किया गया अनुमान सुपरिचित भारतीय परंपराओं के नितांत विरुद्ध है। यह परंपरा महाभारत की रचना को तीन चरणों में विभाजित करती है – (1) जय, (2) भारत और (3) महाभारत और प्रत्येक भाग को अलग-अलग लेखक की कृति बताती है। इस परंपरा के अनुसार व्यास महाभारत के प्रथम संस्कारण के लेखक थे, जिसे ‘जय’ कहा जाता है।
द्वितीय संस्कारण का नाम भारत है। परंपरा इसे वैशम्पायन का लिखा बताती है। यह परंपरा एक पुष्प परंपरा थी। इसकी पुष्टि प्रोफेसर होपकिंस के अनुसंधानों द्वारा होती है, जो महाभारत के अंतसाक्ष्य के परीक्षण पर आधारित है। प्रोफेसर होपकिंस (दि गेट इपिक आफ इंडिया, पृ. 398) के अनुसार महाभारत की रचना कई चरणों में हुई। प्रोफेसर होपकिंस (दि गेट इपिक आफ इंडिया, पृ. 398) का कहना है कि प्रथम चरण में यह केवल पांडु महाकाव्य था। इसमें उपदेशात्मक सामग्री नहीं थी और उसमें उन वीरों से संबंधित कथा और आख्यान थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। प्रोफेसर होपकिंस का कहना है कि यह रचना 400-200 ईसा पूर्व में हुई होगी। दूसरे चरण में इस महाकाव्य की पुनर्रचना हुई और इसमें उपदेश आदि और पुराणों से सामग्री का समावेश किया गया। यह 200 ईसा पूर्व और 200 ईसवी के मध्य हुआ। (1) तीसरे चरण में पहले चरण की कृति को साथ में मिलाकर दूसरे चरण की कृति में बाद के पुराणों को शामिल किया गया, और (2) संवर्द्धित अनुशासन पर्व को शांति पर्व से अलग किया गया है तथा एक अलग पर्व बना दिया गया। यह 200 से 400 ईसवी के बीच हुआ। प्रोफेसर होपकिंस इन तीनों चरणों के अतिरिक्त एक और चरण अर्थात् यदा-कदा हुए विस्तार की अंतिमावस्था बताते हैं। यह 400 ईसवी के बाद मे हुआ। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले प्रो. होपकिंस ने उन सभी तार्कें का अनुमान और उन पर विवेचन कर लिया था, जो श्री तिलक ने दिए हैं, जैसे पाणिनि (दि गेट इपिक आफ इंडिया, पृ. 395) की कृति ओर गृह्य सूत्रों (दि गेट इपिक आफ इंडिया, पृ. 390) में महाभारत का उल्लेख। श्री तिलक ने जो नए साक्ष्य दिए हैं और जिन पर प्रो. होपकिंस ने विचार ही नहीं किया था, वे दो हैं।
इस तरह का पहला साक्ष्य वह है, जिसमें कुछ विवरण दिए गए हैं। इनके बारे में यह बताया जाता है कि ये मेगस्थनीज (गीता रहस्य, पृ. 79) के हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक राजदूत बनकर आया था।
दूसरे साक्ष्य खगोलीय हैं (गीता रहस्य, पृ. 789) जो आदि पर्व में मिलते हैं। इनमें उत्तरायण का उल्लेख है, जो श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ होता है। श्री तिलक ने जो तथ्य मेगस्थनीज के विवरण के आधार पर दिए हैं, उन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता और उनसे यह सिद्ध हो सकता है कि मेगस्थनीज के समय में अर्थात् 300 ईसा पूर्व शौरसैनी समाज में कृष्ण भक्ति संप्रदाय था, परंतु इससे यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि महाभारत की रचना हो चुकी थी। यह नहीं हो सकता। इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि मेगस्थनीज ने जिन आख्यानों-कथाओं का उल्लेख किया है, वे महाभारत से ली गई हैं। इससे यह तो सिद्ध नहीं होता कि ये आख्यान और कथाएं और कहानियां जनसमूह में व्याप्त नहीं थीं और महाभारत के लेखक तथा ग्रीक राजदूत, दोनों ने ही इस अपार सामग्री का चयन नहीं किया था।
श्री तिलक का खगोलीय साक्ष्य काफी ठोस हो सकता है। उनका यह कथन सच है (गीता रहस्य, 2, पृ. 789) कि अनुगीता में यह कहा गया है कि विश्वमित्र ने श्रवण (मा.भा.अश्व. 44.2. और आदि. 71.34) से नक्षत्र की गणना प्रारंभ की थी। समीक्षकों द्वारा इस तथ्य की व्याख्या की गई है और उन्होंने यह बताया है कि उस समय उत्तरायण का प्रारंभ श्रवण नक्षत्र से हुआ था और इसमें मतभेद करना उचित नहीं है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार उत्तरायण धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य के आने पर प्रारंभ होता है। खगोलीय गणना के अनुसार धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य के आने पर उत्तरायण के आरंभ होने का समय शक संवत् शुरू होने के लगभग 1500 वर्ष पूर्व का होना चाहिए, लेकिन खगोलीय गणना के अनुसार उत्तरायण का एक नक्षत्र पूर्व प्रारंभ होने के लिए एक हजार वर्ष का समय लगाता है।
इस गणना के अनुसार उत्तरायण श्रवण नक्षत्र में सूर्य के आने पर प्रारंभ होना चाहिए। यह शक संवत् से पूर्व लगभग 500 वर्ष का समय होता है। यह निष्कर्ष तब उचित था, यदि वह सत्य होता कि संपूर्ण महाभारत एक ग्रंथ के रूप में एक ही समय और एक ही व्यक्ति द्वारा रचा गया था। यह भी बताया गया कि इस अनुमान के लिए कोई प्रमाण नहीं है। अतः श्री तिलक के खगोलीय साक्ष्य के आधार पर महाभारत की रचना-तिथि के निर्धारण में प्रयोग किया जा सकता है, जो इसके द्वारा प्रभावित है। इस प्रसंग में महाभारत का आदि पर्व उल्लेखनीय है। इन्हीं कारणो से महाभारत की रचना की तिथि के संबंध में श्री तिलक का सिद्धांत सटीक नहीं बैठता। वास्तव में महाभारत जैसी कृति के लिए कोई भी एक तिथि के निर्धारण करने का प्रयत्न व्यर्थ ही समझा जाना चाहिए, जो धारावाहिक कथा के रूप में अंतराल देकर दीघ-काल तक लिखा जाता रहा था। हम यही कह सकते हैं कि महाभारत की रचना 400 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसवी तक की गई। इस निष्कर्ष से वह प्रयोजन पूरा नहीं होता, जो श्री तिलक का अभीष्ट है। कुछ विद्वानों को यह अवधि भी बहुत कम लगती है। कहा जाता है (धर्मानंद कोसांबी, हिंदी संस्कृति आणि अहिंसा (मराठी), पृ. 156) कि वन पर्व के 190 वें अध्याय में उल्लिखित एडूको की व्याख्या गलत की गई है और उसका अर्थ बौद्ध स्तूप लगाया गया, जबकि इसका आशय ईदगाहों से है, जिनका निर्माण मुसलमान आक्रमणकारियों ने मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किए गए लोगों के लिए किया था। यदि यह व्याख्या सही है तो इससे यह सिद्ध होगा कि महाभारत के कुछ भाग मौहम्म्द गौरी के आक्रमणों के समय अथवा उसके बाद लिखे गए थे।
अब मैं भगवद्गीता की रचना-तिथि के बारे में श्री तिलक की स्थापनाओं को लेता हूं। वास्तव में उनकी स्थापना में दो तर्क अंतर्निहित हैं। प्रथम, गीता महाभारत का एक भाग है। उन दोनों का रचना-काल एक ही है और वे दोनों ग्रंथ एक ही व्यक्ति के द्वारा रचे गए हैं। उनका दूसरा तर्क यह है कि जो भगवद्गीता आज उपलब्ध है, वह वैसी ही मिलती है, जैसी कि शुरू में लिखी गई थी। मैं इन दोनों तर्कों को अलग-अलग लेता हूं, जिससे कोई भ्रांति न हो।
गीता को महाभारत के साथ उनकी रचना के संबंध में सहयोजित करने में श्री तिलक का उद्देश्य नितांत स्पष्ट है। वह महाभारत के रचना-काल के आधार पर, जो उनके अनुसार ज्ञात है, गीता का रचना-काल निर्धारित करना चाहते हैं, जो अज्ञात है। खेद है कि श्री तिलक ने जिस आधार पर महाभारत और भगवद्गीता के बीच निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है, वह उनके सिद्धांत का सबसे दुर्बल पक्ष है। अगर हम यह स्वीकार करें कि गीता महाभारत का भाग इसलिए है कि इन दोनों ही ग्रंथों के रचयिता व्यास हैं और यही श्री तिलक का तर्क है तो यह कल्पना को सच समझने जैसी बात होगी। इस तर्क में यह स्वीकार कर लिया जाता है कि व्यास किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, जो काफी प्रसिद्ध रहा है। उस तथ्य से स्पष्ट है कि हमारे सम्मुख व्यास महाभारत के रचयिता हैं, व्यास पुराणों के रचयिता हैं। इसलिए यह बात सच नहीं मानी जा सकती कि वही व्यास इन सभी ग्रंथों के रचयिता हैं, जो शताब्दियों तक अलग-अलग लिखे गए। हम सभी जानते हैं कि धार्मिक लेखक अपना नाम छिपाकर उसके बदले किसी पूज्य नाम का उपयोग करके किस प्रकार अपनी कृति को प्रतिष्ठित करा देते हैं और उन दिनों छद्नाम या उपनाम के रूप में व्यास नाम का उपयोग करना उनका स्वभाव बन गया था। यदि गीता के रचयिता व्यास हैं तो कोई दूसरा ही व्यक्ति होना चाहिए, जिसने व्यास नाम का उपयोग किया है।
एक अन्य तर्क भी है, जो भगवद्गीता और महाभारत की एक ही काल में रचना किए जाने के श्री तिलक के सिद्धांत का विरोध करता है। महाभारत में 18 पर्व हैं। इसके अलावा 18 पुराण भी हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि भगवद्गीता में भी 18 अध्याय हैं। प्रश्न यह है कि एक जैसा क्यों हैं? इसका उत्तर यह है कि प्राचीन भारतीय लेखक कुछ नामों और कुछ संख्याओं के बारे में यह समझते थे कि ये अधिक पवित्र हैं। इस तथ्य का उदाहरण व्यास का नाम और 18 की संख्या है, परंतु भगवद्गीता के अध्यायों को 18 तक निर्धारित करने में जो कुछ ऊपरी तौर से दिखता है, उसकी अपेक्षा कोई और विशेष बात है। किसने 18 को पवित्र संख्या निर्धारित किया। क्या महाभारत ने या गीता ने। 18 तक निर्धारित करने में जो कुछ ऊपरी तौर से दिखता है, उसकी अपेक्षा कोई और विशेष बात है। किसने 18 को पवित्र संख्या निर्धारित किया। क्या महाभारत ने या गीता ने? यदि महाभारत ने इसे पवित्र संख्या निर्धारित किया, तब गीता महाभारत के बाद ही रची गई? यदि भगवद्गीता ने इसे पवित्र संख्या निर्धारित किया, तो महाभारत की रचना गीता के बाद होनी चाहिए। स्थिति चाहे कुछ भी क्यों न हो, इन दोनों ग्रंथों की रचना एक ही समय में नहीं की गई होगी।
इस विवेचन को, हो सकता हैं श्री तिलक के पहले प्रस्ताव की दृष्टि से निर्णायक स्वीकार न किया जाए, परंतु एक तर्क है, जिसे मैं निर्णायक समझता हूं। मेरा संकेत महाभारत और भगवद्गीता में कृष्ण की तुलनात्मक स्थिति की ओर है। महाभारत में कृष्ण को कहीं भी भगवान नहीं बताया गया है, जो सभी लोगों को मान्य थे। स्वयं महाभारत में ही दिखाया गया है कि जन-समुदाय कृष्ण को प्रथम स्थान देने के लिए भी तैयार नहीं था। राजसूय यज्ञ में जब धर्मराज ने अतिथियों के सत्कार के समय कृष्ण को प्राथमिकता देनी चाही, तो शिशुपाल ने जो कृष्ण का निकट संबंधी था, कृष्ण का विरोध किया और उन्हें अपशब्द भी कहे। उन्होंने उन्हें निम्न वंश में पैदा हुआ ही नहीं कहा, परंतु उन्हें चरित्रहीन और ऐसा षड़यंत्रकारी कहा, जिसने विजय के लिए युद्ध के नियमों का भी उल्लंघन किया। स्वयं महाभारत के गदा पर्व में इसका उल्लेख है कि कृष्ण के ये कृत्य इतने खराब, लेकिन सत्यतापूर्ण हैं कि जब दुर्योधन कृष्ण के सामने इनका बखान करता है, तब दोषारोपण सुनने के लिए स्वर्ग से देवता आ गए, जो दुर्योधन ने कृष्ण के विरुद्ध किया था और उन अभियोगों के सुनने के बाद उन्होंने अपनी सहमति के प्रतीक स्वरूप पुष्पों की वर्षा की कि ये अभियोग पूर्ण सत्य हैं और सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं। दूसरी ओर भगवद्गीता में कृष्ण को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, पवित्र, प्रिय और सद्गुण के सार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये दोनों रचनाएं, जिनमें एक ही व्यक्तित्व का परस्पर विरोधी आकलन का इस प्रकार से उल्लेख है, एक ही लेखक द्वारा एक ही काल में नहीं लिखी जा सकतीं। खेद की बात है कि श्री तिलक भगवद्गीता को बौद्ध-काल के पूर्व की रचना सिद्ध करते समय इस महत्त्वपूर्ण तथ्य को बिल्कुल ही भूल गए।
श्री तिलक का दूसरा तर्क भी निर्मूल है।भगवद्गीता के रचना-काल को निर्धारित करने का कार्य मृगमरीचिका के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं। इस तर्क की विफलता निश्चित है। इसका कारण यह है कि गीता अकेली पुस्तक नहीं, जिसे एक ही लेखक ने लिखा होगा। इस ग्रंथ में अलग-अलग अध्याय हैं जिन्हें अलग-अलग लेखकों ने अलग-अलग समय पर रचा है।
प्रोफेसर गार्बे एकमात्र ऐसे विद्वान हैं, जिन्होंने इस प्रकार परीक्षण किया जाना आवश्यक समझा है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भगवद्गीता में अलग-अलग चार भाग हैं। वे एक-दूसरे से इतने भिन्न हैं कि आज जिस स्थिति में यह ग्रंथ विद्यमान है, उसमें इन्हें सरलता से निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(1) मूल गीता चारणों द्वारा वर्णित या गाई गई वीर-गाथा मात्र है कि अर्जुन किस प्रकार युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था तथा कृष्ण ने उन्हें युद्ध करने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया और अर्जुन ने यह बात मान ली, आदि-आदि। यह कौतूहल भरी कहानी रही होगी, परंतु इसमें कुछ भी धार्मिक अथवा दार्शनिक नहीं था।
मूल गीता अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 11 के श्लोक 32-33 में मिलती है, जिसमें कृष्ण ने अपने तर्क का समापन इस प्रकार किया है:
मेरे साधन बनो, मेरी इच्छा का पालन करो। युद्ध-जन्य पाप और अनिष्ट की चिंता मत करो, वही करो जैसा कि मैं कहूं। धृष्ट मत बनो।
यही वह तर्क है, जिसका कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए बाध्य करने के लिए प्रयोग किया था और प्रेरणा और आग्रह भरे इसी तर्क ने अर्जुन को राजी कर लिया था। कृष्ण ने संभवतः यह धमकी दी होगी कि अगर उसने युद्ध नहीं किया तो वह बाल का प्रयोग करेंगे। कृष्ण द्वारा अपने विश्व रूप का अहंकार जताना इस बल प्रदर्शन का केवल एक रूप है। इसी सिद्धांत के आधार पर वर्तमान गीता में विश्व रूप से संबंधित अध्याय का मूल भगवद्गीता का एक भाग होना संभव हो सकता है।
(2) मूल भगवद्गीता में प्रथम क्षेपक उसी अंश का एक भाग है, जिसमें कृष्ण को ईश्वर कहा गया है और उन्हें भागवत धर्म में परमेश्वर कहा गया है। गीता का यह भाग वर्तमान भगवद्गीता के उन श्लोकों में मिलता है, जहां भक्ति योग का विवेचन है।
(3) मूल भगवद्गीता में दूसरा क्षेपक वह भाग है, जहां उस पूर्व-मीमांसा के सिद्धांतों की पुष्टि के रूप में सांख्य और वेदांत का वर्णन है, जो उनमें पहले नहीं था। गीता प्रारंभ में एक ऐतिहासिक आख्यान था, जिसमें कृष्ण भक्ति बाद में समाविष्ट कर दी गई। भगवद्गीता में दर्शन संबंधी अंश बाद में जोड़ा गया, यह मूल संवाद की शैली और उसके क्रम से सरलतापूर्वक सिद्ध किया जा सकता है।
अध्याय 1, श्लोक 20-47 में अर्जुन उन कठिनाइयों का वर्णन करते हैं। अध्याय 2 में कृष्ण अर्जुन द्वारा बताई गई कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार तर्क-वितर्क का क्रम चलता है। कृष्ण का प्रथम तर्क श्लोक दो और तीन में दिया गया है, जिसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसका यह आचरण अकीर्तिकर है और आर्य के लिए अशोभनीय है, वह अपुरुषोचित कार्य न करें, यह उसकी मर्यादा के प्रतिकूल है। इस तर्क का अर्जुन ने जो उत्तर दिया है, वह श्लोक 4 से 8 तक वर्णित है।
श्लोक 4 और 5 में अर्जुन कहता है कि ‘मैं भीष्म और द्रोण की हत्या कैसे कर सकता हूं, जो सर्वोच्च आदर के पात्र हैं। इनकी हत्या करने की अपेक्षा भिक्षार्जन करके जीवनयापन करना श्रेयस्कर है। मैं इन वृद्ध और पूज्य जनों का वध कर राज्य-सुख भोगने के लिए जीवनयापन नहीं करना चाहता।’ श्लोक 6 से 8 तक अर्जुन ककहता है, ‘इन दो में क्या श्रेयस्कर है, यह मैं नहीं जानता। क्या हमें कौरवों का समूल नाश करना श्रेयस्कर है अथवा उनके द्वारा हमें पराजित होना श्रेयस्कर है।’ अर्जुन के इस प्रश्न का जो उत्तर कृष्ण ने दिया, वह 11 से 39 तक के श्लोकों में मिलता है। इस उत्तर में कृष्ण यह प्रतिपादित करते हैं। (1) कि शोक करना अनुचित है, क्योंकि सारी वस्तुएं नाशवान होती हैं, (2) यह धारणा असत्य है कि व्यक्ति मर जाता है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है और (3) उसे युद्ध करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना होता है।
जो भी व्यक्ति इस संवाद को पढ़ता है, उसके मन में निम्नलिखित विचार आते हैं:
(1) अर्जुन ने जो प्रश्न प्रस्तुत किए, वे दार्शनिक प्रश्न नहीं हैं। वे स्वाभाविक प्रश्न हैं, जो ऐसे लौकिक व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, जो सांसारिक समस्याओं से जूझ रहा है।
(2) कुछ सीमा तक कृष्ण इन प्रश्नों को स्वाभाविक प्रश्न मानते हैं और इनका नितांत स्वाभाविक उत्तर देते हैं।
(3) यह संवाद एक नया मोड़ ले लेता है। अर्जुन ने जब कृष्ण को यह सूचित कर दिया कि वह निश्चित ही युद्ध नहीं करेगा, तब वह एक नया प्रश्न करता है और यह संदेह व्यक्त करता है कि कौरवों को मारना श्रेयस्कर है अथवा उनके हाथों मारा जाना श्रेयस्कर है। यह परिवर्तन सोद्देश्य किया गया, जिससे कृष्ण युद्ध की दार्शनिक दृष्टि से पुष्टि कर सकें, जो अर्जुन के कथन के संदर्भ में अनावश्यक था।
(4) इसके बाद श्लोक 31 से 38 तक कृष्ण की वाणी मृदु हो जाती है। वह प्रश्न को स्वाभाविक बताते हैं और अर्जुन से युद्ध करने के लिए कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना है।
कोई भी पाठक इससे यह समझ सकता है कि वेदांत-दर्शन का विवेचन नितांत अप्रासंगिक है और बाद में जोड़ा गया है। जहां तक सांख्य-दर्शन का संबंध है, स्थिति बड़ी ही स्पष्ट है। अर्जुन के पक्ष न करने पर भी इसका अक्सर विवेचन किया गया है। जब कभी इसका किसी प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रतिपादन किया गया है, तब उस प्रश्न का युद्ध से कोई संबंध नहीं है। इससे यह पता चलता है कि भगवद्गीता का दार्शनिक अंश मूल गीता का अंश नहीं है, परंतु इसे बाद में जोड़ा गया है और उसे स्थान देने के लिए अर्जुन से कुछ नवीन, समुचित और प्रमुख प्रश्न करवाए गए हैं, जिनका युद्ध की लौकिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं हैं।
(4) मूल भगवद्गीता के तीसरे क्षेपक में वे श्लोक आते हैं, जिसमें कृष्ण को ईश्वर के स्तर से परमेश्वर के स्तर पर पहुंचा दिया गया है। यह क्षेपक अध्याय 10 और 15 में मिलता है।
जैसा कि मैंने कहा था कि भगवद्गीता के रचना-काल का सटीक निर्धारण करना व्यर्थ का कार्य है और इसकी तभी कोई उपयोगिता हो सकती है, जब हर क्षेपक के रचना-काल का पता लगाने की कोशिश की जाए। अगर इस दिशा में प्रयत्न किया जाए, तब, जैसा कि मैंने कहा, दर्शन-रहित मूल गीता महाभारत के मूल पाठ अर्थात् जय का भाग हो सकती है। मूल भगवद्गीता में पहला क्षेपक, जिसमें कृष्ण को ईश्वर के रूप में व्यक्त किया गया है, मेगस्थनीज के कुछ बाद के समय का होना चाहिए, जब कृष्ण केवल जनजातियों के ईश्वर थे (डा. भंडारकर अपनी पुस्तक शैविज्म एंड वैष्णविज्म (शैववाद और वैष्णवाद) में कहते हैं,’यदि वासुदेव कृष्ण की उपासना प्रथम मौर्य सम्राट के राज्य-काल में प्रचलित थी तो यह उपासना मौर्य वंश की स्थापना से बहुत पूर्व काल से ही शुरू हुई होनी चाहिए।’ यह एक ऐसा अपवादित कथन है, जिस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जनजातीय ईश्वर के रूप में कृष्ण और विश्वव्यापी ईश्वर के रूप में कृष्ण के बीच अंतर किया जाना चाहिए। जनजातीय ईश्वर के रूप कृष्ण का वही समय हो सकता है, जिसका सुझाव डा. भंडारकर ने दिया है, लेकिन यह उनके विश्वव्यापी रूप में पूजे जाने का नहीं हो सकता। गीता में यह उनके दूसरे रूप से संबंधित है)। यह कितने बाद का समय है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह काफी बाद का समय होना चाहिए, क्योंकि यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शुरू में कृष्ण मत के प्रति ब्राह्मणों की मैत्री नहीं थी। वस्तुतः वे इसके विरोधी थे (देखें, श्याम शास्त्री मेमोरियल वोल्यूम)। ब्राह्मणों को कृष्ण पूजा स्वीकार करने में कुछ समय अवश्य लगा होगा (कृष्ण मत का विरोध बहुत बाद में शंकराचार्य जैसों ने भी किया)।
मूल भगवद्गीता में दूसरा क्षेपक वह अंश है, जहां सांख्य और वेदांत का विवेचन है। यह जैमिनी और बादरायण के सूत्रों के बाद रखे जाने चाहिए, जिसका कारण दिया जा रहा है। इन सूत्रों के रचना-काल के बारे में प्रो. जैकोबी ने सतर्कतापूर्वक जांच की है (अमेरिकन ओरिएंटल सोसायटी की पत्रिका में दि डेट्स आफ दि फिलोसोफिकल सूत्राज आफ दि ब्राह्मणाज शीर्षक लेख, खंड 31, 1911)। उनका कहना है कि इन सूत्रों की रचना लगभग 200 से 300 ईसवी के बीच हुई।
मूल भगवद्गीता में तीसरा क्षेपक, जहां कृष्ण को ऊंचा उठाकर परमेश्वर का दर्जा दिया है, गुप्त सम्राटों के शासन-काल में जोड़ा गया होगा। इसका कारण स्पष्ट है। जिस प्रकार शक सम्राटों ने महादेव को अपना इष्ट देवता स्वीकार किया था, उसी प्रकार गुप्त वंश के सम्राटों ने कृष्ण-वासुदेव को अपना इष्टदेव स्वीकार कर लिया था। ब्राह्मणों ने, जिनके लिए धर्म एक व्यापार था और जो कभी भी एक ईश्वर के प्रति निष्ठावान नहीं रहे, अपने शासकों को प्रसन्न करने के लिए उन्के इष्टदेव को एक उच्च और शक्तिशाली परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर उसकी पूजा करनी आरंभ कर दी। अगर यह सही व्याखा है, तब मूल भगवद्गीता में यह क्षेपक 400 से 464 ई. के बीच जोड़ा गया होगा।
इन सब प्रमाणों से इस मत को सिद्ध करने में सहायता मिलती है कि भगवद्गीता को बौद्ध धर्म से पूर्व की रचना बताने के प्रयत्न सफल नहीं हो सकते। यह उन लोगों की हवाई कल्पना का नतीजा है, जिनकी बुद्ध और उनके क्रांतिकारी सिद्धांतों के प्रति तिरस्कार की भावना पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है। इतिहास इसे सिद्ध नहीं करता। इतिहास इस बात को बड़ी ही स्पष्टतापूर्वक सिद्ध करता है कि भगवद्गीता के वे अंश, जिनका कुछ सैद्धांतिक महत्त्व है, हर प्रकार से बौद्ध सिद्धांतों और जैमिनी और बादरायण के सूत्रों के काफी बाद के हैं।
रचना-काल के बारे में विवेचन से केवल यही सिद्ध नहीं होता कि भगवद्गीता हीनयान बौद्ध धर्म के, बल्कि यह भी सिद्ध होता है कि महायान बौद्ध धर्म के भी बाद की है। प्रायः लोगों की यह धारणा है कि महायान बौद्ध धर्म का उद्भव बाद में हुआ। कहा जाता है कि इसका उद्भव 100 ईसवी में हुआ, जब कनिष्क ने बौद्ध धर्म में आपसी मतभेद पर निर्णय करने के लिए तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। यह नितांत भ्रम है (इस सारे विषय पर देखिए, ए हिस्टोरिकल स्टडी आफ दि टर्म्स हीनयान एंड महायान और दि ओरिजिन आफ महायान बुद्धिज्म, लेखक रीकन किमूर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1927)। यह कहना सच नहीं कि परिषद होने के बाद बौद्ध धर्म के एक नए संप्रदाय का जन्म हुआ। जो कुछ हुआ, वह यह कि जो लोग वृद्ध हो चले थे, उनके लिए व्यंग्य के रूप में कुछ नए नाम चल पड़े। श्री किमूर का कहना है कि महायान बौद्धों के उस वर्ग का नाम है, जिन्हें महासंघिक कहा जाता था। महासंघिकों का यह संप्रदाय उससे बहुत पहले बन गया था, जितना कि कहा जाता है। अगर जनुश्रुति पर विश्वास किया जाए, तब हम कह सकते हैं कि बुद्ध के परिनिर्वाण के 236 वर्ष बाद अर्थात् 307 (यह तब है, जब बुद्ध की परिनिर्वाण तिथि 543 ईसा पूर्व की मान ली जाए, लेकिन अगर उनकी परिनिर्वाण तिथि 453 ईसा पूर्व मानी जाती है, तब यह 217 ईसा पूर्व होगी) ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में बौद्ध सिद्धांतों को निश्चित करने के लिए हुई प्रथम बौद्ध परिषद के बाद यह अस्तित्व में आया और इस संप्रदाय ने बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय के विरोध का नेतृत्व किया, जिसे बाद में तिरस्कार स्वरूप हीनयान (अर्थात् निम्न पथ के अनुगामी) कहा गया। जिस समय महासंघिकों का, जिन्हें बाद में महायानवादी कहा गया, उदय हुआ, उस समय भगवद्गीता का कहीं पता भी नहीं था।
महायानियों ने भगवद्गीता से क्या ग्रहण किया? वास्तव में ये भगवद्गीता से ग्रहण ही क्या कर सकते थे? जैसा कि श्री किमूर बताते हैं – बौद्ध धर्म के प्रत्येक संप्रदाय की चिंता कम से कम तीन मुख्य सिद्धांतों को लेकर थीं – 1. ऐसे सिद्धांत, जिनमें ब्रह्मांड के अस्तित्व का विवेचन हो, 2. ऐसे सिद्धांत, जिनमें बुद्ध के उपदेशों का विवेचन हो, और 3. जो मानव-जीवन की अवधारणा से संबंधित हों। महायान इसके लिए कोई अपवाद नहीं था। महायान बुद्ध के उपदेशों के अतिरिक्त भगवद्गीता से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता था। विभिन्न सिद्धांतों को लेकर इनके दृष्टिकोण में इतना अंतर है कि वह संभावना भी समय के अंतर के कारण नहीं दिखती।
पूर्ववर्ती विवेचन मेरी स्थापनाके विरुद्ध किए जा सकने वाले अकेले इस आरोप को पूर्णतः खंडित कर देता है, अर्थात् भगवद्गीता अति प्राचीन है, बौद्ध-काल से पहले रची गई थी और इसलिए इसका जैमिनी की पूर्व-मीमांसा से कोई संबध नहीं है और इसमें उनके प्रतिक्रियावादी सिद्धांतों की दार्शनिक आधार पर पुष्टि करने का प्रयत्न नहीं किया गया है।
सार रूप में मेरी स्थापना के तीन पक्ष हैं। दूसरे शब्दों में, इसमें तीन भाग हैं। पहला यह है कि भगवद्गीता मूलतः प्रतिक्रांति की उसी वर्ण की कृति है, जैसी जैमिनी की पूर्व-मीमांसा नामक कृति है-प्रतिक्रांति की अधिकारिक बाइबिल। कुछ लोग अध्याय 2 के 40 से 46 तक श्लोकों का सहारा लेते हैं और यह विचार व्यक्त करते हैं कि भगवद्गीता….।