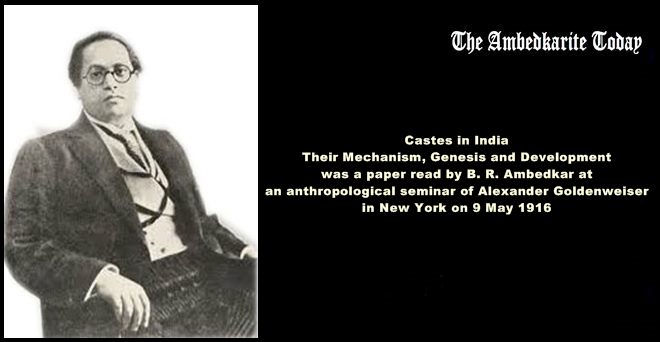भारत में जातिप्रथा/ डॉ. भीमराव आम्बेडकर
Castes in India: Their Mechanism, Genesis and Development was a paper read by B. R. Ambedkar at an anthropological seminar of Alexander Goldenweiser in New York on 9 May 1916. It was later published in volume XLI of Indian Antiquary in May 1917
मैं निःसंकोच कह सकता हूं कि हममें से बहुत लोगों ने स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय देखे होंगे, जो सभ्यता का समग्र रूप प्रस्तुत करते हैं। इस बात पर कुछ लोगों को ही विश्वास आएगा कि संसार में मानव संस्थाओं का प्रदर्शन भी होता है। मानवता-चित्रण विचित्र विचार है, कुछ को यह बात अजीब गोरखधंधा लग सकती है, किंतु नृजाति-विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते आप इस अनुसंधान पर कठोर रुख नहीं अपनाएंगे और कम से कम आपको यह आश्चर्यजनक नहीं लगना चाहिए।
मेरा मानना है कि सबने कुछ ऐतिहासिक स्थल देखे होंगे, जैसे पोम्पियाई के खंडहर और बड़ी उत्कंठा से गाइडों की धाराप्रवाह जबान में इन खंडहरों का इतिहास सुना होगा। मेरे विचार में नृजाति-विज्ञान का विद्यार्थी भी एक मायने में गाइड ही है। वह अपने प्रकृतरूप की तरह (शायद अधिक गांभीर्य और स्व-ज्ञानार्जन की आकांक्षा के साथ) सामाजिक संस्थाओं को यथासंभव निष्पक्षता से देखता है और उनकी उत्पत्ति तथा कार्यप्रणाली का पता लगाता है।
इस गोष्ठी का विचारणीय विषय है – आदिकालीन बनाम आधुनिक बनाम आधुनिक समाज। इसमें भाग लेने वाले मेरे सहयोगियों ने इसी आधार पर आधुनिक या प्रागैतिहासिक संस्थाओं के सार्थक उदाहरण दिए हैं, जिनमें उनका अध्ययन है। अब मेरी बारी है। मेरे आलेख का विषय है-‘भारत में जातिप्रथाः संरचना, उत्पति और विकास।‘
आप जानते हैं कि यह विषय कितना जटिल है, जिसके संबंध में मुझे अपने विचार व्यक्त करने हैं। मुझसे ज्यादा योग्य विद्वानों ने जाति के रहस्यों को खोलने का प्रयास किया है, किंतु यह दुःख की बात है कि यह अभी तक व्याख्यायित नहीं हुआ है और लोगों को इसके बारे में अल्प जानकारी है। मैं जाति जैसी संस्था की जटिलताओं के प्रति सजग हूं और मैं इतना निराशावादी नहीं हूं कि यह कह सकूं कि यह पहेली अगम, अज्ञेय है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि इसे जाना जा सकता है। जाति की समस्या सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से एक विकराल समस्या है। यह समस्या जितना व्यावहारिक रूप से उलझी है, उतना ही इसका सैद्धांतिक पक्ष इन्द्रजाल है। यह ऐसी व्यवस्था है, जिसके फलितार्थ गहन हैं। होने को तो यह एक स्थानीय समस्या है, लेकिन इसके परिणाम बड़े विकराल हैं। जब तक भारत में जातिप्रथा विद्यमान है, तब तक हिन्दुओं में अंतर्जातीय विवाह और बाह्य लोगों से शायद ही समागम हो सके, और यदि हिंदू पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में भी जाते हैं तो भारतीय जात-पांत की समस्या विश्व की समस्या हो जाएगी।
सैद्धांतिक रूप से अनेक महान विद्वानों ने, जिन्होंने श्रम की चाह की खातिर इसके उद्भव तक पहुंचने का प्रयास स्वीकारा था, उनको निराश होना पड़ा। ऐसी स्थिति में मैं इस समस्या का उसकी समग्रता की दृष्टि से समाधान नहीं कर सकता। मुझे आशंका है कि समय, स्थान और कुशाग्रता मुझे असफल कर देगी, यदि मैंने इस समस्या को वर्गीकृत न करके अपनी सीमाओं से अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। जिन पक्षों को मैं निरूपति करना चाहता हूं, वे हैं, जातिप्रथा की संरचना, उत्पत्ति और इसका विकास। मैं इन्हीं सूत्रों तक अपने आपको सीमित रखूंगा, केवल आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण देते हुए ही विषयांतर करूंगा। विषय का प्रतिपादन करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि प्रसिद्ध नृजाति-विज्ञानियों के अनुसार, भारतीय समाज में आर्यों, द्रविड़ों, मंगोलियों और शकों का सम्मिश्रण है। ये जातियां देश-देश से शताब्दियों पूर्व भारत पहुंचीं और अपने मूल देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ यहां बस गईं। तब इनकी स्थिति कबायली वाली थी। ये अपने पूर्ववर्तियों को धकेल कर इस देश के अंग बन गए। इनके परस्पर सतत संपर्कों और संबंधों के कारण एक समन्वित संस्कृति का सूत्रपात हुआ, परंतु भारतीय समाज के विषय में यह बात कहना असंगत है कि वह विभिन्न जातियों का संकलन है। पूरे भारत में भ्रमण करने पर दिक्दिगंत में यह साक्ष्य मिलेगा कि इस देश के लोगों में शारीरिक गठन और रंग-रूप की दृष्टि से कितना अंतर है। संकलन से सजातीयता उत्पन्न नहीं होती है। यदि रक्त-भेद की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय समाज विजातीय है, हां यह संकलन सांस्कृतिक रूप से अत्यंत गुंथा हुआ है। इसी आधार पर मेरा कहना है कि इस प्रायद्वीप को छोड़कर संसार का कोई देश ऐसा नहीं है, जिसमें इतनी सांस्कृतिक समरसता हो। हम केवल भौगोलिक दृष्टि से ही सुगठित नहीं हैं, बल्कि हमारी सुनिश्चित सांस्कृतिक एकता भी अविच्छिन और अटूट है, जो पूरे देश में चारों दिशाओं में व्याप्त है। इसी सांस्कृतिक एकरूपता के कारण जातिप्रथा इतनी विकराल समस्या बन गई है कि उसकी व्याख्या करना कठिन कार्य है। यदि हमारा समाज केवल विजातीय या सम्मिश्रण भी होता, तब भी कोई बात थी, किंतु यहां तो सजातीय समाज में भी जातिप्रथा घुसी हुई है। हमें इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के साथ-साथ इसके संक्रमण की भी व्याख्या करनी होगी।
आगे विश्लेषण करने से पूर्व हमें जातितंत्र की प्रकृति पर भी विचार करना होगा। मैं नृजाति-विज्ञान के कुछ विद्वानों की परिभाषाएं प्रस्तुत करना चाहता हूं –
1. जाति के संबंध में फ्रांसीसी विद्वान श्री सेनार का सिद्धांत है-तीव्र वंशानुगत आधार पर घनिष्ठ सहयोग, विशिष्ट पारंपारिक और स्वतंत्र संगठनों से युक्त, जिसमें एक मुखिया और पंचायत हो, उसकी समय-समय पर बैठकें होती हों, कुछ उत्सवों पर मेले हों, एक सा व्यवसाय हो, जिसका विशिष्ट संबंध रोटी-बेटी व्यवहार से और समारोह अपमिश्रण से हो और इसके सदस्य उसके अधिकार क्षेत्र से विनियमित होते हों, जिसका प्रभाव लचीला हो, पर जो संबंद्ध समुदाय पर प्रतिबंध और दंड लागू करने में सक्षम हो और सबसे बढ़कर समूह से अपरिवर्तनीय।
2. नेसफील्ड जाति की परिभाषा इस प्रकार करते हैं – समुदाय का एक वर्ग, जो दूसरे वर्ग से संबंधों का बहिष्कार करता हो और अपने संप्रदाय को छोड़कर दूसरे के साथ शादी-व्यवहार तथा खान-पान से परहेज करता हो।
3. सर एच. रिजले के अनुसार-जाति का अर्थ है, परिवारों का या परिवार समूहों का संगठन, जिसका साझा नाम हो, जो किसी खास पेशे से संबंद्ध हो, जो एक से पौराणिक पूर्वजों-पितरों के वंशज होने का दावा करता हो, एक जैसा व्यवसाय अपनाने पर बल देता हो और सजातीय समुदाय का हामी हो।
4. डा.केतकर ने जाति की परिभाषा इस प्रकार की है- दो लक्षणों वाला एक सामाजिक समूह, (क) उसकी सदस्यता उन लोगों तक सीमित होती है, जो जन्म से सदस्य होते हैं और जिनमें इस प्रकार जन्म लेने वाले शामिल होते हैं; (ख) कठोर सामाजिक कानून द्वारा सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह करने के लिए वर्जित किए जाते हैं।
हमारे लिए इन परिभाषाओं की समीक्षा अत्यावश्यक है। यह स्पष्ट है कि अलग-अलग देखने पर तीन विद्वानों की परिभाषाओं में बहुत कुछ बाते हैं या बहुत कम तत्व हैं। अकेले देखने में कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं और मूल भाव किसी में भी नहीं है। उन सबने एक भूल की है कि उन्होंने जाति को एक स्वतंत्र तत्व माना है, उसे समग्र तंत्र के एक अंक के रूप में नहीं लिया है। फिर भी सारी परिभाषाएं एक-दूसरे की पूरक हैं, जो तथ्य एक विद्वान ने छोड़ दिया है, उसे दूसरे ने दर्शाया है। मैं केवल उन सूत्रों पर विचार रखूंगा और उनका मूल्यांकन करूंगा, जो उपर्युक्त परिभाषाओं के अनुसार सभी जातियों में समान रूप से पाए जाते हैं, जो जाति की खासियत माने जाते हैं।
हम सेनार से शुरू करते हैं। वह अपमिश्रण की बात करते हैं और यह बताते हैं कि यह जाति की प्रकृति है। इसे देखते हुए यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि यह किसी जाति से संबंधित नहीं है। यह आमतौर पर पूजा-समारोहों से संबंद्ध बात है और शुद्धता के सामान्य सिद्धांत का पोषक तत्व है। परिणामस्वरूप इसका संबंध जाति से नहीं है और इसकी कार्यप्रणाली को ध्वस्त किए बिना, इसको प्रतिरुद्ध किया जा सकता है। अपमिश्रण का सिद्धांत जाति से जोड़ दिया गया है, क्योकि जो जाति सर्वोच्च कही जाती है, वह पुरोहित वर्ग है।
हम जानते हैं कि पुरोहित और पवित्रता का पुराना संबंध है। सार यही है कि अपमिश्रण का सिद्धांत तभी लागू होता है, जब किसी जाति का धार्मिक स्वभाव हो। श्री नेसफील्ड अपने तरीके से कहते हैं कि जाति की प्रकृति है कि उनके साथ खान-पान नहीं किया जाता, जो उनकी जाति के बाहर हैं। यह नया तथ्य है, फिर भी ऐसा लगता है कि श्री नेसफील्ड इस व्यवस्था के प्रभाव से अपरिचित हैं। चूंकि जाति अपने में ही सीमित एक संस्था है, अतः वह सामाजिक अंतरंगता के विरुद्ध है, जिसमें खान-पान आदि पर भी पाबंदी है। परिणाम यह निकलता है कि बाहरी लोगों से खान-पान पर पाबंदी सकारात्मक निषेध का कारण नहीं है, बल्कि जातिप्रथा परिणाम है अर्थात् भिन्नता का गुरुमंत्र है। इसमें कोई संदेह नहीं कि खान-पान पर प्रतिबंध भिन्नता के कारण नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक व्यवस्था है, परंतु यह तत्व बाद में जुड़ा है। सर एच. रिजले ने विशेष ध्यान देने योग्य कोई बात नहीं कही है।
अब हम डा.केतकर की परिभाषा का विश्लेषण करते हैं। उन्होंने इस विषय को और विशद् रूप दिया है। केवल यही बात नहीं है कि वह भारत के निवासी हैं, बल्कि उन्होंने विवेचनात्मक और पैनी दृष्टि से निष्पक्ष राय दी है, जो जातिप्रथा के बारे में उनके अध्ययन के कारण हुआ है। उनकी परिभाषा विचारणीय है, क्योंकि उन्होंने जातितंत्र का विश्लेषण जातिप्रथा के आधार पर किया है और अपना ध्यान केवल उन्हीं लक्षणों तक केंद्रित रखा है, जो जातिप्रथा के अंतर्गत जाति के अस्तित्व में अनिवार्य है। उन्होंने फालतू बातों की ठीक अवहेलना की है, जो गौण और क्षणिक हैं। उनकी परिभाषा के बारे में कहा जा सकता है कि उनके विचरों में कहीं थोड़ी भ्रांति है, वैसे उनमें विशदता और स्पष्टता है। वह रोटी-बेटी के व्यवहार में भेदभाव की बात कहते हैं। मेरा कहना है कि मूल बात एक ही है, रोटी से भी परहेज है और बेटी व्यवहार से भी, पर डा.केतकर ने बताया है कि ये हैं एक ही सिक्के के दो पहलू। यदि आप बेटी व्यवहार पर पाबंदी लगाते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि आप परिधि संकुचित कर लेते हैं। इस प्रकार ये दोनों लक्षण एक ही पदक के मुख्य भाग तथा पृष्ठ भाग हैं।
जातितंत्र के इस समीक्षात्मक मूल्यांकन से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि सजातीय विवाह का निषेध या ऐसे विवाह का न पाया जाना ही जातिप्रथा का मूल है, परंतु अमूर्त नृविज्ञान के आधार पर कुछ ऐसे लोग इस बात को नकार सकते हैं, क्योंकि सजातीय विवाह के पक्षधर वर्ग जातीय समस्या बढ़ाए बिना ऐसा कर सकते हैं। सामान्यतः यह संभव है, क्योंकि यह एक मूर्त सत्य है कि सजातीय विवाह समर्थक समाज सांस्कृतिक रूप से भिन्न रहकर अलग बस्तियों में बस सकता है, जहां एक-दूसरे से कोई मतलब न हो। इस बारे में एक युक्तिसंगत उदाहरण दिया जा सकता है कि अमरीकन भारतीयों के नाम से विख्यात नीग्रो समुदाय और गोरों के विभिन्न कबीले अमरीका में मौजूदा हैं, परंतु हमें इस संबंध में भ्रांति नहीं रहनी चाहिए कि भारत में स्थिति भिन्न है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भारत में सजातीय प्रथा है। भारत की विभिन्न प्रजातियां कुछ खास क्षेत्रों में निवास करती हैं और उनका आपस में मेल-जोल है तथा उनमें सांस्कृतिक एकता है, जो सजातीय समाज का एकमात्र मापदंड है। ऐसी सजातीयता को आधार मानने से जातिप्रथा एक नयी समस्या का रूप धारण करती है, जो केवल सजातीय विवाह समर्थक समाज या कबीलों से अलग स्थिति है। भारत में जातिप्रथा का अर्थ है समाज को कृत्रिम हिस्सों में विभाजित करना, जो रीति-रिवाजों और शादी व्यवहार की भिन्नताओं से बंधे हों। परिणाम स्पष्ट है कि सजातीय विवाह एकमात्र लक्षण है, जो जातिप्रथा की विशेषता है और यदि हम यह जताने में सफल हो जाएं कि सजातीय विवाह ही क्यों होते हैं तो हम व्यावहारिक रूप से यह साबित कर सकते हैा कि जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका ताना-बाना क्या है?
अब आप भलीभांति समझ सकते हैं कि मैं सजातीय विवाह को जातिप्रथा की जड़ क्यों मानता हूं। मैं आपको पशोपेश में डालना नहीं चाहता। मैं इस पर प्रकाश डालता हूं।
यहां यह बताना असंगत न होगा कि आज दुनिया का कोई अन्य सभ्य देश ऐसा नहीं है, जो आदिम मान्यताओं से लिपटा हो। इस देश का धर्म आदिम है और इसके आदिम संकेत इस आधुनिक काल में भी पूरे जोर-शोर से इस पर हावी हैं। इस सिलसिले में मैं बहिर्गोत्र विवाह का उल्लेख करना चाहता हूं। आदिम युग में बहिर्गोत्र विवाहों का प्रचलन सर्वविदित है। युग परिवर्तन के साथ-साथ तो इस शब्द की सार्थकता ही जाती रही और रक्त के घनिष्टतम रिश्ते को छोड़कर इस संबंध में विवाहों पर कोई प्रतिबंध ही नहीं रहा, लेकिन भारत में आज भी बहिर्गोत्र विवाह प्रथा ही प्रचलित है। भारतीय समाज में आज भी कबीला प्रथा मौजूद है, हालांकि कबीले नहीं रहे। विवाह पद्धति इसका प्रमाण है, जो बहिर्गोत्र प्रथा पर आधारित है। यहां सपिंड विवाहों पर ही प्रतिबंध नहीं है, बल्कि सगोत्र विवाह भी अपवित्र माने जाते हैं।
इसलिए आपको सबसे महत्त्वपूर्ण बात याद रखनी है कि सजातीय प्रथा भारत के लिए विदेशी प्रथा है। भारत में विभिन्न गोत्र हैं और ये बहिर्गोत्र विवाह से संबंधित हैं। ऐसे ही अन्य वर्ग भी हैं, जो टोटम अर्थात् देवों को मानते हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत में बहिर्गोत्र विवाह एक विधान है और इसका उल्लंघन संभव नहीं, यहां तक कि जात भीतर विवाह प्रथा के बावजूद, गोत्र बाहर विवाह पद्धति का कठोरता से पालन किया जाता है। गोत्र वाहर विवाह करने की प्रथा का उल्लंघन करने पर जात बाहर विवाह करने वालों की तुलना में कठोर दंड का विधान है। आप देख सकते हैं कि बहिर्गोत्र विवाह का नियम बना दिया जाए तो जातिप्रथा का आधार ही मिट जाए, क्योंकि बहिर्गोत्र का अर्थ परस्पर विलय है, परंतु हमारे यहां जातिप्रथा है। परिणाम यही निकता है कि जहां तक भारत का संबंध है, यहां बहिर्गोत्र विवाह विधान से अंततः जाति अर्थात् सजातीय विवाह विधान भी जुड़ा है। बहरहाल, मूल रूप से बहिर्गोत्री समाज में सजातीय विवाह विधान का पालन सरलता से संभव है, जो जातिप्रथा का मूल है और गंभीर समस्या है। इसी विधान के माध्यम से बहिर्गोत्र विवाहों के रहते सजातीय विवाह होता है। इसी पर विचार करके हमें अपनी समस्या का समाधान मिल सकता है।
इस प्रकार सजातीय विवाह प्रथा की बहिर्गोत्रीय विवाहों पर जकड़ ही जातिप्रथा का कारक है, लेकिन बात इतनी सरल नहीं। हम मान लेते हैं कि एक ऐसा समुदाय है, जो एक जाति बनाना चाहता है और विचार करता है कि सजातीय विवाह प्रथा के प्रचलन के लिए कौन सा माध्यम अपनाए। यदि कोई समुदाय सजातीय विवाह पद्धति को दरकिनार करके अंतरजातीय विवाह निषेध का उल्लंघन करता है और अपने समुदाय के बाहर विवाह रचा लेता है, तो वह व्यर्थ है। विशेष रूप से इस परिप्रेक्ष्य में कि सजातीय विवाह प्रथा के पहले सभी विवाह बहिर्गोत्र होते थे। फिर सभी वर्गों में यह प्रकृति है कि वे सम्मिश्रण के पक्षधर हैं और वे एक सजातीय वर्ग में संगठित हो जाते हैं। यदि इस प्रकृति का प्रतिकार किया जाए तो यह आवश्यक है कि जिन वर्गों के बीच विवाह संबंध नहीं हैं, उन्हें भी प्रतिबंधित वर्ग में सम्मिलित किया जाए। इसके लिए आवश्यक है, परिधि का बढ़ाया जाना।
इसके बावजूद बाहरी समुदाय में शादी-व्यवहार को रोक देने से आंतरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनका समाधान सरल नहीं हैं। मोटे तौर पर सभी वर्गों में स्त्री-पुरुष संख्या समान होती है और समान वय के स्त्री-पुरुष में बराबरी भी होती हैं, किंतु समाज उन्हें बराबर नहीं मानता। साथ ही जो समुदाय जाति-संरचना करता है, उसमें स्त्री-पुरुष समानता परम लक्ष्य होता है। इसके बिना सजातीय विवाह प्रथा सफल नहीं हो सकती। इसी तथ्य को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि यदि सजातीय विवाह प्रथा को बनाए रखना है, तो आंतरिक दृष्टि से दांपत्य अधिकारों का विधान रखना होगा, अन्यथा समाज के लोग दायरे से बाहर हो जाएंगे। यदि आंतरिक दृष्टि से दांपत्य अधिकार दिए जाते हैं तो जाति-संरचना की सफलता के लिए स्त्री-पुरुष संख्या समान रखनी आवश्यक होगी। दोनों के बीच भारी संख्या विषमता होने से सजातीय विवाह प्रथा चरमरा उठेगी।
जातियों की समस्या के समाधान के लिए विवाह योग्य स्त्री-पुरुष की असमानता को रोकना होगा। प्रकृति इसमें सहायक तभी हो सकती है, जब पति के साथ पत्नी या पत्नी के साथ पति की मृत्यु हो जाए। इससे ही संतुलन बना रह सकता है। ऐसा असंभव है। वास्तव में, पति के मरने पर पत्नी बच जाती है और पत्नी के मरने पर पति बचा रह जाता है। इस प्रकार इन बचे रहे स्त्री-पुरुषों की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि कोई बचा हुआ पुरुष या स्त्री-जाति के बाहर विवाह करके जाति-व्यवस्था के जाल को छिन्न-भिन्न कर दे। यदि उन्हें स्वतंत्र रहने दिया गया और उन्हें नव-युगल बनाने का कोई नियम नहीं बनता है तो इस प्रकार के अतिरिक्त स्त्री-पुरुष बचे रहेंगे। ऐसे यह बहुत संभव है कि वे सीमाएं लांघ जाएं तथा बाहर विवाह रचा लें और जाति में विजातीय लोगों को भर लें।
अब हम यह देखें कि जिस वर्ग की हमने ऊपर कल्पना की है, वह इन बचे हुए स्त्री-पुरुष का क्या करेगा। पहले हम विधवा स्त्रियों को लेते हैं। उनका दो तरह से इंतजाम किया जा सकता है, जिससे कि सजातीय विवाह प्रथा बनी रहे।
पहलाः उसे उसके मृत पति के साथ जला दिया जाए और उससे मुक्ति पा ली जाए। स्त्री-पुरुष अंतर को घटाने के लिए यह एक अव्यावहारिक तरीका है। कुछ मामलों में यह संभव है, कुछ में नहीं। नतीजा यह निकला कि प्रत्येक स्त्री को ठिकाने नहीं लगाया जा सकता। वैसे यह एक आसान तरीका है, लेकिन बहुत कटु स्थिति है। इस तरह विधवाएं यदि ठिकाने नहीं लगाई जा सकें और वे जाति में ही बनी रहें, तो दुहरा खतरा पैदा हो जाता है। वह जात बाहर विवाह कर लेगी और सजातिवाद को तिलांजलि दे देगी या मुकाबलेबाजी में अपनी जाति की उन स्त्रियों का हक मार लेगी, जो विवाह योग्य हैं। इस तरह यह खतरा है। यदि वह उसके पति के साथ जलाई न जा सके तो उसका कुछ इंतजाम करना होगा।
दूसरा निराकरण है कि उन्हें हमेशा के लिए विधवा रहने दिया जाए। जहां तक वांछित परिणाम का संबंध हैं, उसे जला देना सदा विधवा बनाए रखने से बेहतर है। जला देने से तीनों आशंकाएं, जिनका विधवा को सामना करना पड़ता है, नष्ट हो जाती हैं। मरने से वह कोई समस्या नहीं रहेंगी और वह न जाति बाहर और नही जाति में पुनर्विवाह करेगी, परंतु उसे विधवा रूप में जीवित रहने देना, जलाने से अच्छा और व्यावहारिक भी है। जहां यह अपेक्षाकृत मानवीय प्रथा है, इससे पुनर्विवााह की आशंका भी टलती है, परंतु इससे उस वर्ग की नैतिकता स्थापित नहीं रह सकती। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनिवार्य वैधव्य में स्त्री बच जाती है, परंतु पूरे जीवन उसे किसी की वैध पत्नी बनने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इससे अनैतिकता के लिए रास्ते खुलते हैं, लेकिन यह कोई दुःसाध्य कार्य नहीं है। उसे इस हालत में लाया जा सकता है कि उसमें आकर्षण लेशमात्र भी न बचे।
जाति-संरचना करने वाले समुदाय में बचे पुरुषों (विधुरों) की समस्या अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह विधवाओं की अपेक्षा अधिक विकराल है। इतिहास के आरंभ से ही पुरुष का स्त्री की अपेक्षा अधिक महत्त्व रहा है। इसका प्रभुत्व हर समाज में रहा है। इसकी प्रतिष्ठा अधिक रही है। पुरुष की परंपरागत श्रेष्ठता के कारण उसकी इच्छाओं का सदा सम्मान किया जाता रहा है। दूसरी आरे नारी सदा धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं का शिकार होती रही है। इस हालत में विधवाओं के साथ वैसा ही बर्ताव नहीं किया गया है, जैसा बचे हुए पुरुषों (विधुर) के साथ किया गया है।
उसे उनकी मृत पत्नी के साथ जला डालना दो कारणों से खतरनाक है। पहली बात तो यह है कि ऐसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि वह पुरुष है। दूसरे यदि ऐसा किया जाए तो एक तगड़ा व्यक्ति जाति की खातिर लुप्त हो जाएगा। अब उसने आसानी से निबटने के लिए दो विकल्प रह जाते हैं। मैं इन्हें आसान विकल्प इसलिए कह सकता हूं, क्योंकि वह समाज के लिए उपयोगी हैं।
वह समाज के लिए कितना ही महत्त्वपूर्ण हो, सजातीय विवाह इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है और इसलिए समाधान ऐसा होना चाहिए, जो इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति करे। ऐसी परिस्थितियों में उसे भी विधवा की तरह आजीवन विधुर रहने के लिए बाध्य या मेरे विचार में ऐसा करने के लिए राजी किया जा सकता है। यह समाधान बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि कुछ बिना विवश किए भी आत्म-संयम बरत सकते हैं या वे इससे भी चार कदम आगे बढ़कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं, लेकिन मानव प्रकृति को देखते हुए ऐसी अपेक्षा आसानी से पूर्ण नहीं हो सकेगी। दूसरी स्थिति में संभव है कि ऐसा व्यक्ति समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने पर उसके नैतिक सिद्धांतों के लिए खतरा बन सकता है।
दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर यद्यपि ब्रह्मचर्य व्रत उन मामलों में आसान है, जहां इसे सफलता से अपनाया जाता है, लेकिन फिर भी जाति की भौतिक सुख-समृद्धि के लिए लाभदायक नहीं है। यदि वह सही अर्थों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और सांसरिक सुखों का त्याग कर देता है, तो वह जाति के नैतिक मूल्यों या सजातीय विवाह के लिए खतरा नहीं होगा, जैसा कि उसके सांसारिक जीवन बिताने पर होता। जहां तक भौतिक सुख-समृद्धि का प्रश्न है, ब्रह्मचारी की तरह जीवनयापन करने वाला व्यक्ति जला दिए गए व्यक्ति के समान है। प्रभावी सौहार्दपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों की निर्धारित संख्या होनी चाहिए।
विधुरों पर ब्रह्मचर्य थोपना सैद्धांतिक और व्यावहारिक, दोनों दृष्टियों से विफल रहा है। यह जाति के हित में है कि गृहस्थ रहे। समस्या केवल यह है कि उसे जाति में से ही पत्नी सुलभ कराई जाए। शुरू में इसमें कठिनाई होती है, क्योंकि जातियों में स्त्री और पुरुष का अनुपात एक-एक का है। इस तरह किसी के दोबारा विवाह की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि जब जातियों की परिधियां बनी होती हैं तो विवाह योग्य पुरुषों और स्त्रियों की संख्या पूरी तरह संतुलित होती है। इन परिस्थितियों में विधुर को जाति में रखने के लिए उसका पुनर्विवाह उन बालिकाओं से किया जा सकता है, जो अभी विवाह योग्य न हों। विधुरों के लिए यह यथा संभव उपाय है। इस प्रकार वह जाति में बना रहेगा। इस प्रकार उनके जाति से बाहर निकलने और उनकी संख्या में कमी को रोका जा सकेगा और सजातीय विवाह वाले समाज में नैतिकता भी बनी रहेगी।
यह स्पष्ट है कि ऐसे चार तरीके हैं, जिन्हें अपनाने से स्त्री-पुरुषों में संख्या का अनुपात बनाए रखा जा सकता है – (1) स्त्री को उसके मृत पति के साथ सती कर दिया जाए, (2) उसे आजीवन विधवा रखा जाए, जो जलाने से कुछ कम पीड़ादायक है, (3) विधुरों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने को बाध्य किया जाए, और (4) विधुर का ऐसी लड़की से विवाह कर दिया जाए, जिसकी आयु अभी विवाह योग्य न हों। हालांकि मेरे उपरोक्त विचार के अनुसार विधवा को जलाना और विधुर पर ब्रह्मचर्य व्रत थोपना सजातीय विवाह को बनाए रखने क लिए समूह के प्रयत्नों के प्रति संदेहास्पद सेवा होगी, लेकिन जब साधनों को शक्ति के रूप में स्वतंत्र किया जाता है अथवा उन्हें गतिमान कर दिया जाता है, तो वे लक्ष्य बनते हैं। तब फिर वे साधन कौन सा लक्ष्य प्राप्त करते हैं। वे सजातीय विवाह की व्यवस्था को जारी रखते हैं, जबकि विभिन्न परिभाषाओं के हमारे विश्लेषण के अनुसार सजातीय विवाह और जाति एक ही बात है। अतः इन साधनों का अस्तित्व और जाति समरूप हैं तथा जाति में इन साधनों का समावेश है।
मेरे विचार में जाति-व्यवस्था में यह जाति की सामान्य क्रियाविधि है। अब हम अपना ध्यान इन उच्च सिद्धांतों से हटाकर हिंदू समाज में विद्यमान जातिप्रथा और उसकी क्रियाविधि की जांच में लगाएं। मैं निःसंकोच कह सकता हूं कि अतीत के रहस्यों को खोलने वालों के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं और निःसंदेह भारत में जाति-व्यवस्था अति प्राचीन संस्था है। इन हालात में यह और भी ज्वलंत यथार्थ है कि जहां तक हिन्दुओं का संबंध है, उनके बारे में कोई आधिकारिक या लिखित संकेत नहीं हैं तथा भारतीयों का दृष्टिकोण ऐसा बन गया है कि वह इतिहास लेखन को मूर्खता मानते हैं, क्योंकि उनके लिए जगत मिथ्या है, लेकिन ये संस्थाएं जीवित रहती हैं, यद्यपि चिरकाल तक इनका लिखित प्रमाण नहीं रहता और उनके रीति-रिवाज व नैतिक मूलय अवशेषों की भांति अपने आप में एक इतिहास हैं। हम अपने कर्तव्य में सफल होंगे, यदि हम अतिरेक पुरुष और अतिरेक स्त्री से संबंधित समस्याओं का हिन्दुओं द्वारा जो निदान किया गया है, उसकी जांच करें।
सतही तौर पर देखने वाले व्यक्ति को हिंदू समाज की सामान्य क्रियाविधि जटिल लगे, किंतु वह स्त्रियों से संबंधित तीन असाधारण रीतियां प्रस्तुत करती हैं, ये हैं –
1. सती या विधवा को उसके मृत पति के साथ जलाना।
2. थोपा गया आजीवन वैधव्य , जिसके अंतर्गत एक विधवा को पुनःविवाह करने की आज्ञा नहीं हैं।
3. बालिका विवाह।
संन्यास के बाद भी विधु में विकट लिप्सा होती हैं, परंतु कुछ मामलों में यह शुद्ध मानसिक कारणों से ही संभव है।
जहां तक मैं समझता हूं, आज तक इन प्रथाओं के उद्भव की कोई वैज्ञानिक व्याख्या सामने नहीं आई है। अनेक दार्शनिक सिद्धांत इन प्रथाओं की प्रतिष्ठा में प्रतिपादित किए गए हैं, परंतु कहीं से इनके उद्भव और अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता। सती सम्माननीय है (ए.के. कुमार स्वामीः सतीः ए डिफेंस ऑफ द ईस्टर्न वीमेन इन द सोशियोलोजिकल रिव्यू, वोल्यूम, 6,1913) क्योंकि यह पति-पत्नी के बीच शरीर और आत्मा की संपूर्ण एकात्मकता और श्मशान से परे तक समर्पण को दर्शाती है, क्योंकि इसमें पत्नीत्व को साकार रूप दिया गया है, जैसा कि उमा ने अच्छी तरह उस समय स्पष्ट किया है, जब उन्होंने कहा था,” हे महेश्वर, अपने पतिदेव के लिए नारी का समर्पण ही उसका सम्मान है, यही उसका शाश्वत स्वर्ग है। भावुकता में वह आगे कहती हैं, मेरी धारणा है कि यदि आप मुझसे संतुष्ट नहीं हैं तो मेरे लिए स्वर्ग की कामना करना बेकार हैं। आजीवन वैधव्य क्यों सम्माननीय है, मैं नहीं जानता, न ही मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला है, जो इसकी प्रशंसा करता हो, हालांकि पालन करने वाले अनेकानेक हैं। बालिका विवाह की प्रशंसा में डा.केतकर कहते हैं, एक सच्चे आस्थावान स्त्री अथवा पुरुष को विवाह सूत्र में बंधने के बाद अन्य पुरुष-स्त्री से लगाव नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की पवित्रता न केवल विवाह के उपरोंत, बल्कि विवाह पूर्व भी आवश्यक है, क्योंकि चारित्र्य का केवल यही सही आदर्श है। किसी अपरिणता को पवित्र नहीं माना जा सकता, यदि वह उस व्यक्ति के अलावा जिससे उसका विवाह होने वाला है, किसी अन्य व्यक्ति से प्रणय करती है। यदि वह ऐसा करती है तो यह पाप है। इसलिए एक लड़की के लिए यह अच्छा होगा कि कामवासना जाग्रत होने से पूर्व उसे यह पता होना चाहिए कि उसे किससे प्रेम करना है।(हिस्ट्री आफ कास्ट इन इंडिया, 1909, पृ. 2-33) तब उसका विवाह किया जाए।
ऐसी हवाई और कुतर्क की बातें यह तो प्रमाणित करती हैं कि ऐसी प्रथाओं को क्यों सम्मानित किया गया, परंतु हमें यह नहीं बतातीं कि ये रिवाज कैसे पड़े। मेरा यह मानना है कि इनको सम्मान देने का कारण ही यह है कि इन्हें अपनाया गया। जिस किसी को भी 18वीं शताब्दी के व्यक्तिवाद का थोड़ा-सा भी ज्ञान होगा, वह मेरे कथन का सार समझ जाएगा। सदा से यह प्रथा रही है कि आंदोलनों का सर्वोपरि महत्त्व होता है। बाद में उन्हें न्याय-संगत बनाने के लिए और उन्हें नैतिक बल देने के लिए उन्हें दार्शनिक सिद्धांतों का संबल दे दिया जाता है। इसी तरह मैं निवेदन करता हूं कि इसी कारण इन रिवाजों की प्रशंसा की गई, क्योंकि इनके चलन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशंसा की जरूरत थी। प्रश्न यह है कि ये कैसे बढ़े? मेरा विचार है कि जाति-संरचना में इनकी आवश्यकता थी और उनको लोकप्रिय बनाने के लिए सिद्धांतों की बैसाखी पकड़ा दी गई। हम जानते हैं कि ये रिवाज कितने क्रूर, कष्टकारी और घातक हैं। रिवाज साधन मात्र हैं, जबकि उन्हें आदर्श घोषित किया गया, परंतु यह हमें परिणामों के बारे में भ्रमित नहीं कर सकते। सरलता से कहा जा सकता है कि साधनों को आदर्श बना देना आवश्यक होता है और इस मामले में तो खासतौर से उन्हें भारी प्रेरणा देकर उत्साहित किया जाता है। साधन को साध्य मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, किंतु हम अपने साधन की प्रकृति नहीं बदल सकते। आप कानून बना सकते हैं कि सभी बिल्लियां-कुत्ते हैं, जैसे अप किसी साधन को उद्देश्य मान सकते हैं, परंतु आप साधन की प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते। अतः आप बिल्लियों को कुत्ते नहीं बना सकते। ठीक ऐसे ही साधन को साध्य मान सकते हैं। इसी कारण मेरा यह कहना ठीक है कि साधन और साध्य को एकाकर कर दियाजाए, परंतु यह कैसे उचित ठहराया जा सकता है कि जातिप्रथा और सजातीय विवाह प्रथा के लिए सतीप्रथा, आजीवन विधवा अवस्था और बालिका विवाह, विधवा स्त्री, और विधुर पुरुष की समस्या के समाधान हैं। सजातीय विवाह-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये रिवाज आवश्यक हैं, जबकि सजातीय विवाह प्रथा के अभाव में जातिप्रथा का अस्तित्व बने रहना संदेहास्पद हैं।
भारत में जातिप्रथा के प्रचलन और संरक्षण की क्रियाविधि पर विचार करते हुए अगला प्रश्न यह है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। इसके मूल का प्रश्न एक कड़वा प्रश्न है और जातपांत के अध्ययन में इसी दुखद अवहेलना की गई है। कुछ ने इसका समर्थन किया है और कुछ ने इस प्रयत्न पर जानबूझकर पर्दा डाल दिया है। कुछ लोग समझ पाने में सफल रहे हैं कि जात-पांत का मूल कहां हो सकता है। वे कहते हैं, यदि हम मूल के प्रति अपनी स्नेह भावना पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो हमें उसके बहुवचन रूप अर्थात् ‘जात-पांत के मूल’ का प्रयोग करना चाहिए। वैसे भारत में जात-पांत के मूल के बारे में कोई उलझन पेश नहीं हुई है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि सजातीय विवाह ही जातपांत का एकमात्र कारण है और जब में जाति के मूल की बात कहता हूं तो इसका अर्थ सजातीय विवाह प्रथा की क्रियाविधि के मूल से हैं।
किसी समाज में व्यक्तियों की अतिसूक्ष्म अवधारणा को इतने शक्तिशाली ढंग से प्रचारित करना-मैं गंदगी उछालना कहने जा रहा था। यह राजनीतिक भाषा में कोरी बकवास है। यह बात नगण्य है कि व्यक्ति मिलकर समाज बनाते हैं। समाज सर्वथा वर्गों से मिलकर बनता है; इसमें वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर बल देना अतिश्योक्ति हो सकती है, परंतु यह सच है कि समाज में कुछ निश्चित वर्ग होते हैं। आधार भिन्न हो सकते हैं। वे वर्ग आर्थिक, आध्यात्मिक या सामाजिक हो सकते हैं, लेकिन समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वर्ग से संबंद्ध होता है। यह एक शाश्वत सत्य है और आरंभिक हिंदू समाज भी इसका अपवाद नहीं रहा होगा। जहां तक हम जानते हैं, वह अपवाद नहीं था। यदि हम इस सामान्य नियम को ध्यान में रखते तो पाते हैं कि जातपांत की उत्पति के अध्ययन में यह बहुत उपयोगी तत्व साबित हो सकता है, क्योंकि हम यह निश्चित करना चाहते हैं कि वह कौन सा वर्ग था, जिसने सबसे पहले अपनी जाति की संरचना की। इसीलिए वर्ग और जाति एक-दूसरे के दो रूप है। फर्क सिर्फ यह है कि जाति अपने को सजातीय परिधि में रचने वाला वर्ग है।
जातिप्रथा के मूल का अध्ययन हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है कि वह कौन-सा वर्ग है, जिसने इस परिधि का सूत्रपात किया, जो इसका चक्रव्यूह है? यह प्रश्न बहुत कौतूहलजनक है, परंतु यह बहुत प्रासंगिक है और इसका उत्तर उस रहस्य पर से पर्दा हटाएगा कि पूरे भारत में जातिप्रथा कैसे पनपी और दृढ़ होती गई। दुर्भाग्य से इस प्रश्न का सीधा उत्तर मेरे पास नहीं हैं। मैं इसका परोक्ष उत्तर ही दे सकता हूं। मैंने अभी कहा है कि विचाराधीन रीति-रिवाज हिंदू समाज में प्रवाहित हैं। तथ्यों को यथार्थ बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि कथन को स्पष्ट किया जाए, ताकि इसकी व्यापकता पर प्रकाश डाला जा सके। यह प्रथा अपनी पूरी दृढ़ता के साथ केवल एक जाति अर्थात ब्राह्मणों में प्रचलित है, जो हिंदू समाज की संरचना में सर्वोच्च स्थान पर है और गैर-ब्राह्मण जातियों ने इसका केवल अनुसरण किया, जहां इसके पालन में न तो उतनी दृढ़ता है और न संपूर्णता।
यह महत्त्वपूर्ण तथ्य हमारे सम्मुख महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर सकता है। यदि गैर-ब्राह्मण जातियां इस प्रथा का अनुसरण करती हैं, जैसा कि आसानी से देखा जा सकता है, तो यह प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि कौन-सा वर्ग जाति-व्यवस्था का जन्मदाता है। ब्राह्मणों ने क्या अपने लिए एक परिधि बनाई और जाति की संरचना कर ली, यह एक अलग प्रश्न है, जिस पर किसी अन्य अवसर पर विचार किया जाएगा, परंतु इस रीति-नीति पर कड़ाई से पालन और इस पुरोहित वर्ग द्वारा प्राचीन-काल से इस प्रथा का कड़ाई से अमल, यह प्रमाणित करता है कि वही वर्ग इस अप्राकृतिक संस्था का जन्मदाता था। उसने अप्राकृतिक साधनों से इसकी नींव डाली और इसे जिंदा रखा।
अब मैं अपने लेखन के तीसरे भाग पर आता हूं, जिसका संबंध पूरे भारत में जातपांत के उद्भव और विस्तार से है। जिस प्रश्न का मुझे उत्तर देना है, वह यह कि देश के अन्य गैर-ब्राह्मण समुदायों में यह प्रथा कैसे फैली? इसके उत्तर में मेरा विचार है कि पूरे भारत में जातिप्रथा के प्रचलन से ज्यादा पीड़ादायक इसके उद्भव का प्रश्न है। जैसा कि मैं समझता हूं, इसका मुख्य कारण यह है कि इसका विस्तार और सूत्रपात दो अलग-अलग बातें नहीं हैं। विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि जातिप्रथा या तो भोले-भाले समाज पर कानून गढ़ने वालों ने नैतिकता का मुलम्मा चढ़ाकर थोप दी या फिर सामाजिक विकास की भक्त भारतीय जनता में किसी नियम के अधीन पनपती रही।
पहले मैं भारत के विधि-निर्माता के बारे में बताना चाहूंगा। हर देश में उसके विधि-निर्माता होते हैं, जो अवतार कहलाते हैं, ताकि आपातकाल में पापी समाज को सही दिशा दी जा सके। यही विधि-निर्माता कानून और नैतिकता की प्रतिस्थापना करते हैं। भारत में विधि-निर्माता के रूप में यदि मनु का कोई अस्तित्व रहा है, तो वह एक ढीठ व्यक्ति रहा होगा। यदि यह बात सत्य है कि उसने स्मृति अथवा विध की रचना की तो मैं कहता हूं कि वह दुःसाहसी व्यक्ति था और जिस मानवता ने उसके विधान को शिरोधार्थ किया, वह वर्तमान-काल की मानवता से भिन्न थी। यह अकल्पनीय है कि जाति-विधान की संरचना की गई। यह कहना कोई अतिश्योक्ति न होगी कि मनु ने ऐसा कोई विधान नहीं बनाया कि एक वर्ण को इतना रसातल में पहुंचा दिया कि उसे पशुवत बना दिया और उसको प्रताड़ित करने के लिए एक शिखर वर्ण गढ़ दिया। यदि वह क्रूर न होता, जिसने सारी प्रजा को दास बना डाला, तो ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वह अपना आधिपत्य जमाने के लिए इतने अन्यायपूर्ण विधान की संरचना करता, जो उसकी ‘व्यवस्था’ में साफ झलकता है।
मैं मनु के विषय में कठोर लगता हूं, परंतु यह निश्चित है कि मुझमें इतनी शक्ति नहीं कि मैं उसका भूत उतार सकूं। वह एक शैतान की तरह जिंदा है, किंतु मैं नहीं समझता कि वह सदा जिंदा रह सकेगा। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मनु ने जाति के विधान का निर्माण नहीं किया और न वह ऐसा कर सकता था। जातिप्रथा मनु से पूर्व विद्यमान थी। वह तो उसका पोषक था, इसलिए उसने उसे एक दर्शन का रूप दिया, परंतु निश्चित रूप से हिंदू समाज का वर्तमान रूप जारी नहीं रह सकता। प्रचलित जातिप्रथा को ही उसने संहिता का रूप दिया और जाति-धर्म का प्रचार किया। जातिप्रथा का विस्तार और उसकी दृढ़ता इतनी विराट है कि यह एक व्यक्ति या वर्ग की धूर्तता और बलबूते का काम नहीं हो सकता। तर्क में यह सिद्धांत है कि ब्राह्मणों ने जाति-संरचना की। मैंने मनु के विषय में जो कहा है, मैं इससे अधिक और नहीं कहना चाहता, सिवाय यह कहने के कि वैचारिक दृष्टि से यह गलत और इरादतन दुर्भावनापूर्ण है। ब्राह्मण और कई बातों के लिए दोषी हो सकते हैं, और मैं निःसंकोच कह सकता हूं कि वे हैं भी, परंतु गैर-ब्राह्मण अन्य जन -समुदायों पर जातिप्रथा थोपना उनके बूते के बाहर की बात थी। अपने इस तरह के दर्शन द्वारा, हो सकता है उन्होंने अपने ही तरीके से इस प्रक्रिया को पनपने में सहायता की हो, परंतु अपनी क्षमता से वे अपनी योजना कार्यान्वित नहीं करा सकते थे। चाहे कोई कितना भी गौरवशाली हो! चाहे कोई कितना ही कठोर क्यों न हों! अपने ढंग से समाज को चलाने में वह प्रशंसित तो हो सकता है, किंतु यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चलता। मेरी आलोचना की तीव्रता अनावश्यक लग सकती है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह असत्य नहीं है। पुरातन पंथी हिन्दुओं के मन में दृढ़ धारणा है कि हिंदू समाज किसी तरह जातिप्रथा की प्रणाली में ढल गया और यह संस्था शास्त्रों ने बनाई है। यह विश्वास केवल विद्यमान ही नहीं है, बल्कि उसे इस आधार पर न्यायसंगत भी ठहराया जाता है। यह स्थिति सुखद हो सकती है, क्योंकि यह शास्त्रों से जन्मी है और शास्त्र गलत नहीं हो सकते। मैंने इस प्रकृति की विसंगतियों की ओर इस आधार पर ही ध्यान नहीं दिलाया है कि वैज्ञानिकता के नाम पर धार्मिक सामान्यताएं थोप दी गईं, न ही मैं उन सुधारकों का पक्षधर हूं, जो इसके विरुद्ध है। यह प्रथा उपदेशों से बड़ी है और न ही उपदेश इसे उखाड़ सकते हैं। मैं इस प्रकृति की निस्सारता बताना चाहता हूं, जिसने धार्मिक प्रतिबंधों को वैज्ञानिक कहकर ओढ़ रखा हैं।
इस तरह व्यक्ति-पूजा का सिद्धांत भारत में जातिप्रथा के प्रचलन के निराकरण में बहुत लाभदायक साबित नहीं होता। पश्चिमी विद्वानों ने संभवतः व्यक्ति पूजा को विशेष महत्त्व नहीं दिया, लेकिन उन्होंने दूसरी व्याख्याओं को आधार बना लिया। उनके अनुसार भारत में जिन मान्यताओं ने जातिप्रथा को जन्म दिया है, वे हैं (1) व्यवसाय, (2) विभिन्न कबायली संगठनों का प्रचलन, (3) नयी धारणाओं का जन्म, (4) संकर जातियां
प्रश्न यह उठता है कि क्या वे मान्यताएं अन्य समाजों में मौजूद नहीं हैं और क्या भारत में ही उनका विशिष्ट रूप विद्यमान है। यदि वे भारत की विशेषताएं नहीं हैं और पूरे विश्व में एक समान हैं, तो उन्होंने भूमंडल के किसी अन्य भाग में जातियां क्यों नहीं गढ़ लीं? क्या इसका कारण यह है कि वे देश वेदों की भूमि की अपेक्षा अधिक पवित्र हैं या विद्वान गलती पर हैं? मैं सोचता हूं कि बाद की बात सही है।
अनेक लेखकों ने किसी न किसी मान्यता के आधार पर अपनी-अपनी विचारधारा के समर्थन में उच्च सैद्धांतिक मूल्यों के दावे किए हैं। कोई विवशता प्रकट करते हुए कहता है कि गहराई से देखने पर प्रकट होता है कि ये सिद्धांत उदाहरणों के सिवाय कुछ भी नहीं हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड का कहना है कि इसमें महानता का कुछ सार न होते हुए भी महान नाम जुड़े हुए हैं। सर डेनजिल इब्बतसन, नेसफील्ड, सेनार और सर एच.रिजले के सिद्धांत यही हैं। मोटे तौर पर इनकी आलोचना में यह कहा जा सकता है कि यह लीक पीटने का प्रयत्न है। नेसफील्ड उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सिर्फ कार्य, केवल कार्य ही वह आधार था, जिस पर भारत की जातियों की पूर्ण प्रथा का निर्माण हुआ। लेकिन उन्हें यह बताना होगा कि वह इस कथन से हमारी जानकारी में कोई इजापुा नहं करते, जिसका सार यही है कि भारत में जातियों का आधार व्यवसाय मात्र है और यह स्वयं में एक लचर दलील है। हमें नेसफील्ड महोदय से इस सवाल का जवाब चाहिए कि यह कैसे हुआ कि विभिन्न व्यवसायी वर्ग विभिन्न जातियां बन गए? मैं अन्य नृजाति-विज्ञानियों के सिद्धांतों पर विचार करने के लिए सहर्ष प्रसन्न होता, यदि यह सही न होता कि नेसफील्ड का सिद्धांत एक अजीब सिद्धांत है।
मैं इन सिद्धांतों की आलोचना जारी रखते हुए इस विषय पर अपनी बात रखना चाहूंगा कि जिन सिद्धांतों ने जातिप्रथा को विभाजनकारी नियमों के पालन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बताया है, जैसा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने विकास के सिद्धांत में व्याख्या की है और इसे स्वाभाविक बताया है तथा इसे ‘जैविक संरचना भेद‘ कहकर लचर पुरातनपंथी शब्द जाल की धारणाओं को पुष्ट किया है या सुजनन-विज्ञान के प्रयत्नों का समर्थन किया है, जिससे उसकी सनक का आभास होता है कि जातिप्रथा अवश्यंभावी है या विधि-सम्मत है, यह जानकर निरीह वर्गों पर सजग होकर इन नियमों को आरोपित किया गया है।
यह उचित ही रहेगा कि शुरू में मैं यह बात कहूं कि अन्य समाजों के समान भारतीय समाज भी चार वर्णों में विभाजित था, ये हैं (1) ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग, (2) क्षत्रिय या सैनिक वर्ग, (3) वैश्य अथवा व्यापारिक वर्ग, (4) शूद्र अथवा शिल्पकार और श्रमिक वर्ग। इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि आरंभ में यह अनिवार्य रूप से वर्ग विभाजन के अंतर्गत व्यक्ति दक्षता के आधार पर अपना वर्ण बदल सकता था और इसीलिए वर्णों को व्यक्तियों के कार्य की परिवर्तनशीलता स्वीकार्य थी। हिंदू इतिहास में किसी समय पुरोहित वर्ग ने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया और इस तरह स्वयं सीमित प्रथा से जातियों का सूत्रपात हुआ। दूसरे वर्ण भी समाज विभाजन के सिद्धांतानुसार अलग-अलग खेमों में बंट गए। कुछ का संख्या बल अधिक था तथा कुछ का नगण्य। वैश्य और शूद्र वर्ण मौलिक रूप से वे तत्व हैं, जिनकी जातियों की अनगिनत शाखा, प्रशाखाएं कालांतर में उभरी हैं, क्योंकि सैनिक व्यवसाय के लोग असंख्य समुदायों में सरलता से विभाजित नहीं हो सकते, इसलिए यह वर्ण सैनिकों और शासकों के लिए सुरक्षित हो गया।
समाज का यह उप-वर्गीकरण स्वाभाविक है, किंतु उपरोक्त विभाजन में अप्राकृतिक तत्व यह है कि इससे वर्णों में परिवर्तनशीलता के मार्ग अवरुद्ध हो गए और वे संकुचित बनते चले गए, जिन्होंने जातियों का रूप ले लिया। प्रश्न यह उठता है कि क्या उन्हें अपने दायरे में रहने के लिए विवश किया गया और उन्होंने सजातीय विवाह का नियम अपना लिया या उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा किया। मेरा कहना है कि इसका द्विपक्षीय उत्तर है- कुछ ने द्वार बंद कर लिए और कुछ ने दूसरे के द्वार अपने लिए बंद पाए। पहला पक्ष मनोवैज्ञानिक है और दूसरा चालाकी भरा, परंतु ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं और जाति-संरचना की संपूर्ण रीति-नीति में दोनों की व्याख्या जरूरी है।
मैं पहले मनोवैज्ञानिक व्याख्या से शुरू करता हूं। इस संबंध में हमें इस प्रश्न का उत्तर खोजना है कि औद्योगिक, धार्मिक या अन्य कारणों से वर्ग अथवा जातियों ने अपने आपको आत्म-केंद्रित या सजातीय विवाह की प्रथा में क्यों बांध लिया? मेरा कहना है कि ब्राह्मणों के करने के कारण ऐसा हुआ। सजातीय विवाह या आत्म-केंद्रित रहना ही हिंदू समाज का चलन था और क्योंकि इसकी शुरुआत ब्राह्मणो ने की थी, इसलिए गैर-ब्राह्मण वर्गों अथवा जातियों ने भी बढ़-चढ़कर इसकी नकल की और वे सजातीय विवाह प्रथा को अपनाने लगे। यहां यह खरबूजे को देखकर खरबूजे के रंग बदलने वाली कहावत चरितार्थ होती है। इसने सभी उप-विभाजनों को प्रभावित किया। इस तरह जातिप्रथा का मार्ग प्रशस्त हुआ। मनुष्य में नकलबाजी की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। इस कारण भारत में जातिप्रथा के जन्म की यह व्याख्या पर्याप्त हैं। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि बाल्टर बागेहोट को कहना पड़ा, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह नकलबाजी स्वैच्छिक होती है या इसके पीछे कोई भावना काम कर रही होती है। इसके विपरीत, इसका जन्म मानव के अवचेतन मन में होता है और पूर्ण चेतना जागने पर उसके प्रभावों का आभास होता है। इस तरह इसके तत्काल उदय का प्रश्न नहीं है, बल्कि बाद में भी इसका अहसास नहीं होता है। दरअसल, हमारी नकल करने की प्रवृत्ति का स्रोत विश्वास होता है और ऐसे कारण हैं, जो पूर्वकालीन रूप से हमें यह विश्वास कराते हैं तथा हमें विश्वास करने से विरक्त करते हैं – यह हमारी प्रकृति के अस्पष्ट भाग हैं। सरल मन से नकल करने की प्रवृत्ति पर कोई संदेह नहीं है। (फिजिक्स एंड पालिटिक्स (भौतिकी एवं राजनीति शास्त्र) 1915, पृष्ठ 60)
नकल करने की इस प्रवृत्ति के विषय को गेबरिल टार्डे ने वैज्ञानिक अध्ययन का रूप दिया, जिन्होंने नकल करने की प्रवृत्ति को तीन नियमों में बांटा है। उसके तीन नियमों से एक है कि नीचे वाले ऊपर की नकल करते हैं। उन्हीं के शब्दों में, अवसर मिलने पर दरबारी सदा अपने नायकों, अपने राजा या अधिपति की नकल करते हैं और आम जनता भी उसी प्रकार अपने सामंतों की नकल करती है (लॉज ऑफ इमीटेशन (नकल करने के सिद्धांत), अनुवाद : ई.सी. पार्सन्स, पृ. 217)। नकल के बारे में टार्डे का दूसरा नियम है कि चाहे आदर्श पात्र और अनुसरणकर्ता के बीच कितनी ही दूरी क्यों न हों, उनके अनुसार नकल करने की इच्छा और तीव्रता में कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हीं के शब्दों में, जिस व्यक्ति की नकल की जाती है, वह होता है हमारे बीच सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति या समाज। दरअसल, जिन्हें हम श्रेष्ठ मानते हैं, उनसे हमारा अंतर कितना ही हो, यदि हम उनसे सीधे संपर्क में आते हैं तो उनका संसर्ग अत्यंत प्रभावोत्पादक होता है। अंतर का अर्थ समाज-विज्ञान के आधार पर लिया गया है। यदि हमारा उनसे प्रतिदिन बार-बार संसर्ग होता है और उनके जैसे रंग-ढंग अपनाने का अवसर मिलता है, तो वह व्यक्ति चाहे हमसे कितने ही ऊंचे स्तर का क्यों न हो, कितना ही अपरिचित हो, फिर भी हम स्वयं को उसके निकट मानते हैं। सबसे कम दूरी पर निकटतम व्यक्ति के अनुसरण का नियम प्रकट करता है कि ऊंची हैसियत वाले व्यक्ति निरंतर सहज प्रभाव छोड़ते हैं (लॉज ऑफ इमीटेशन (नकल करने के सिद्धांत), अनुवाद : ई.सी. पार्सन्स, पृ. 225)।3
हालांकि प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, परंतु अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कुछ जातियों की संरचना नकल से हुई। मुझे लगता है कि यह जाना जाए कि हिंदू समाज में नकल करके जातियां बनाने की परिस्थितियां हैं या नहीं? इस नियम के अनुसार नकल करने की गुंजाइश इस प्रकार है 1.जिस स्रोत की नकल की गई है, उसकी समुदाय में प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और (2) समुदाय के सदस्यों में प्रतिदिन और अनेक बार संपर्क होने चाहिए। भारतीय समाज में ये परिस्थितियां मौजूद हैं, इसमें कोई शकर नहीं है। ब्राह्मण अर्द्ध देवता माना जाता है और उसे अंशावतार जैसा कहा जाता है। वह विधि नियोजित करता है और सभी को उसके अनुसार ढालता है। उसकी प्रतिष्ठा असंदिग्ध है और वह शीर्ष परमानंद है। क्या शास्त्रों द्वारा प्रायोजित और पुरोहितवाद द्वारा प्रतिष्ठिा ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालने में विफल हो सकता है? यदि यह कहानी सही है तो उसके बारे में यह विश्वास क्यों किया जाता है कि वह जातिप्रथा की उत्पत्ति का कारण है। यदि वह सजातीय विवाह का पालन करता है तो क्या दूसरों को उसके पद चिह्नों पर नहीं चलना चाहिए। निरीह मानवता! चाहे वह कोई दार्शनिक हो या तुच्छ गृहस्थ, उसे इस गोरखधंधे में फंसना ही पड़ता है, यह अवश्यंभावी है। अनुसरण सरल है, आविष्कार सरल है, आविष्कार कठिन।
जातिप्रथा की संरचना में दूसरों से सीखने की प्रवृत्ति की कितनी भूमिका है, यह बताने के लिए गैर-ब्राह्मण वर्गों की प्रवृत्ति को समझना होगा, जिनके लिए आज तक इस प्रथा के पोषक रीति-रिवाज विद्यमान हैं, हिंदू मस्तिष्क को इन्होंने जकड़ रखा है और उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, सिवाय सतत विश्वास भाव के, जैसे एक पोखर में जलकुंभी। एक तरीके से हिंदू समाज में सती प्रथा, बालिका विवाह और विधवा की यथास्थिति जातियों की हैसियत के हिसाब से विद्यमान है, परंतु इन प्रथाओं का चलन विभिन्न जातियों में असमान है, जिससे उन जातियों का भेद परिलक्षित होता है (मैं भेद शब्द का प्रयोग टार्डियन अर्थ में कर रहा हूं)। जो जातियां ब्राह्मणों के निकट हैं, वे इन तीनों प्रथाओं की नकल का कड़ाई से पालन करती हैं। दूसरे जो इनसे कुछ कम निकट हैं, उनमें केवल वैधव्य और बालिका विवाह प्रचलित हैं; अन्य जो कुछ और दूरी पर हैं, उनमें केवल बालिका विवाह प्रमुख हैं तथा सबसे अधिक दूरी वाले लोग जातिप्रथा के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। मैं निःसंदेह कह सकता हूं कि यह अधूरी नकल इसी प्रकार है, जैसे टार्डे ने ‘दूरी’ बताई हैं। आंशिक रूप से यह प्रथाओं का पाश्विक लक्षण है। यह स्थिति टार्डे के नियम का पूर्ण उदाहरण है और इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भारत में जातिप्रथा निम्न वर्ग द्वारा उच्च वर्ग की नकल का प्रतिफल है। इस स्थान पर मैं अपने ही पूर्वोक्त कथन की पुनरावृत्ति करना चाहूंगा, जो आपके सम्मुख अनायास और बिना समर्थन के उपस्थित हुआ होगा। मैंने कहा था कि इन विचाराधीन तीन प्रथाओं के बल पर ब्राह्मणों ने जातिप्रथा की नींव डाली। उस विचार के पीछे मेरा तर्क यही था कि इन प्रथाओं को अन्य वर्गों ने वहीं से सीखा है। गैर-ब्राह्मण जातियों में इन रिवाजों की ब्राह्मणों जैसी नकल-प्रवृत्ति की भूमिका पर प्रकाश डालने के बाद मेरा कहना है कि ये प्रवृत्ति उनमें आज भी मौजूद है, चाहे वे अपनी इस आदत से परिचित भी न हों। यदि इन वर्गों ने किसी से सीखा है तो इसका अर्थ है कि समाज में उन प्रथाओं का किसी न किसी वर्ग में प्रचलन रहा होगा और उसका दर्जा काफी ऊंचा हुआ होगा, तभी वह दूसरों का आदर्श हो सकता है, परंतु किसी ईश्वरवादी समाज में कोई आदर्श नहीं हो सकता, सिर्फ ईश्वर का सेवक हो सकता है।
इसमें उस कहानी की पूर्णाहुति हो जाती है कि जो निर्बल थे, जिन्होंने अपने को अलग कर लिया। हमें अब यह देखना है कि दूसरों ने अपने लिए उनके दरवाजे बंद देखकर अपना घर क्यों बंद कर लिया। इसे मैं जातिप्रथा के निर्माण की क्रियाविधि की प्रक्रिया मानता हूं। यही कारीगरी थी, क्योंकि ऐसा अवश्यंभावी होता है। यही दृष्टिकोण और मानसिकता है, जिसके कारण हमारे पूर्ववर्ती इस विषय की व्याख्या करने से कतरा गए, क्योंकि उन्होंने जाति को ही एक अलग ईकाई मान लिया, जबकि वह जातिप्रथा का ही एक अंग होती है। इस चूक या इस पैनी दृष्टि के अभाव के कारण ही सही अवधारणा बनने में मदद नहीं मिली है। अतः सही व्याख्या करने की आवश्यकता है। एक टिप्पणी के जरिए मैं अपनी व्याख्या प्रस्तुत करूंगा, जिसे कृपया आप सदा ध्यान में रखें। वह टिप्पणी इस प्रकार है;: जाति अपने आप में कुछ नहीं है, उसका अस्तित्व तभी होता है, जब वह सारी जातियों में स्वयं भी एक हिस्सा हो। दरअसल, जाति कुद है ही नहीं, बल्कि जातिप्रथा है। मैं इसका उदाहरण देता हूं, अपने लिए जाति-संरचना करते समय ब्राह्मणों ने ब्राह्मण इतर जातियां बना डालीं। अपने तरीके से मैं यह कहूं कि अपने आपको एक बाड़े में बंद करके दूसरों को बाहर रहने के लिए विवश किया। एक दूसरे उदाहरण से मैं अपनी बात स्पष्ट करूंगा।
भारत को संपूर्ण रूप से देखें, जहां विभिन्न समुदाय हैं और सबको अपने समुदाय से लगाव है, जैसे हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई और पारसी, लेकिन हिन्दुओं को छोड़कर शेष में आंतरिक जातिभेद नहीं हैं। परंतु एक-दूसरे के साथ व्यवहार में उनमें अलग-अलग जातियां हैं। यदि पहले चार समुदाय अपने को अलग कर लेंगे तो पारसी अपने आप ही बाहर रह जाएंगे, परंतु परोक्ष रूप से वे भी आपस में अलग समुदाय बना लेंगे। सांकेतिक रूप से कहना चाहता हूं कि यदि ‘क’ सजातीय विवाह पद्धति में सीमित रहना चाहता है, तो निश्चित रूप से ‘ख’ को भी विवश होकर अपने में ही सिमट कर रह जाना पड़ेगा।
अब यही बात हम हिंदू समाज पर भी लागू करें, आपके सामने एक व्याख्या पहले से मौजूद हें कि निजद्वैतवाद के परिणामस्वरूप जो प्रवृत्ति इस समाज को विरासत में मिली है, वह है पृथकतवाद। मेरे इस नए विचार से नैतिकतावादियों की भृकुटि चढ़ सकती हैं, जातपांत की धार्मिक या सामाजिक संहिता जाति विशिष्ट के लिए असाध्य हो सकती है। किसी जाति के उद्दंड सदस्यों को यह आशंका होती है कि उन्हें मनचाही जाति में शामिल होने का विकल्प न देकर, जाति-बहिष्कृत कर दिया गया है। जाति के नियम बहुत कठोर होते हैं और उनके उल्लंघन की माप का कोई पैमाना नहीं होता है। नयी विचारधारा एक नयी जाति बना देती है, क्योंकि पुरातन जातियां नवीनता को सह नहीं पाती। अनिष्टकारी विचारकों को गुरु मानकर प्रतिष्ठित किया जाता है। जो अवैध प्रेम संबंधों के दोषी होते हैं तो वे भी उसी दंड के भागी होंगे। पहली श्रेणी उनकी है, जो धार्मिक समुदाय से जाति बनाते हैं, दूसरे वे हैं, जो संकर जाति बनाते हैं। अपनी संहिता का उल्लंघन करने वालों को दंड देने में कोई सहानुभूति नहीं अपनाई जाए। यह दंड होता है, हुक्का-पानी बंद और इसकी परिणति होती है – एक पृथक जाति की रचना। हिंदू मानसिकता में यह कमियां नहीं होतीं कि हुक्का-पानी बंद के भागी अलग होकर एक अलग जाति बना लें। इसके विपरीत वे लोग नतमस्तक होकर उसी जाति में रहकर बने रहना चाहते हैं (बशर्ते कि उन्हें इसकी इजाजत दे दी जाए) परंतु जातियां सिमटी हुई इकाइयां हैं और जानबुझकर उनमें यह चेतना होती है कि बहिष्कृत लोग एक अलग जाति बना लें। इसका विधान बड़ा निर्दयी है और इसी बल के अनुपालन का परिणाम है कि उन्हें अपने में सिमटना पड़ता है, क्योंकि अन्य वर्गों ने अपने को ही परिधि में करके अन्य वर्गों को बाहर बंद कर दिया है, जिसका परिणाम है कि नए समुदाय (जातिगत नियमों के निंदनीय आधार पर निर्मित समुदाय) यंत्रवत् विधि द्वारा आश्चर्यजनक बहुलता के साथ जातियों के बराबर परिवर्तन किए गए हैं। भारत में जाति-संरचना की प्रक्रिया की यह दूसरी कहानी बताई गई है।
अतः मुख्य सिद्धांत का समापन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जातिप्रथा का अध्ययन करने वालों ने कई गलतियां की हैं, जिन्होंने उनके अनुसंधान को पथभ्रष्ट कर दिया। जातिप्रथा का अध्ययन करने वाले यूरोपियन विद्वानों ने व्यर्थ ही इस बात पर जोर दिया है कि जातिप्रथा रंग के आधार पर बनाई गई, क्योंकि वे स्वयं रंगभेद के प्रति पूर्वाग्रही हैं। उन्होंने जाति समस्या का मुख्य तत्व यही भेद माना है, परंतु यह सत्य नहीं है। डा.केतकर ने सही कहा है कि सभी राजा, चाहे वे तथाकथित आर्य थे अथवा द्रविड, आर्य कहलाते थे। जब तक विदेशियों ने नहीं कहा, भारत के लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं रहा कि कोई कबीला या कुटुंब आर्य है या द्रविड़। चमड़ी का रंग इस देश में जाति का मानदंड नहीं रहा (हिस्ट्री आफ कास्ट पृ. 82)।
वे अपनी व्याख्या का विवरण देते रहे और इसी बात पर सिर पटकते रहे कि जातिप्रथा के उद्भव का यही सिद्धांत हैं। इस देश में व्यावसायिक और धार्मिक आदि जातियां हैं, यह सत्य है, परंतु किसी भी हालत में उनका सिद्धांत जातियों के मूल से मेल नहीं खाता। हमें यह पता लगाना है कि व्यावसायिक वर्ग जातियां क्यों हैं? इस प्रश्न को कभी छुआ ही नहीं गया। अंतिम परिणाम यह है कि उन्होंने जाति-समस्या को बहुत आसान करके समझा, जैसे वे चुटकी बजाते ही बन गई हों। इसके विपरीत जैसा मैंने कहा है यह मान्य नहीं हैं, क्योंकि इस प्रथा में बहुत जटिलताएं हैं। यह सत्य है कि जातिप्रथा की जड़ें आस्थाएं हैं, परंतु आस्थाओं के जाति संरचना में योगदान के पहले ही ये मौजूद थीं और दृढ़ हो चुकी थीं। जाति-समस्या के संबंध में मेरे अध्ययन के चार पक्ष हैं : (1) हिंदू जनसंख्या में विविध तत्वों के सम्मिश्रण के बावजूद इसमें दृढ़ सांस्कृतिक एकता है, (2) जातियां इस विराट सांस्कृतिक इकाई का अंग हैं, (3) शुरू में केवल एक ही जाति थी, और (4) इन्हीं वर्गों में देखी-देखी या बहिष्कार से विभिन्न जातियां बन गईं।
आज भारत में जाति-समस्या ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है, क्योंकि इस अप्राकृतिक विधान को तिलांजलि देने के लिए सतत प्रयत्न हो रहे हैं। सुधार के ये प्रयत्न जातियों के मूल से संबंधित विवादों से उत्पन्न हुए हैं कि क्या यह प्रथा सर्वोच्च स्तर के आदेशों से हुई या विशिष्ट परिस्थितियों में मानव समाज के सहज विकास का प्रतिफल है। जो व्यक्ति बाद के विचार के पक्षधर हैं, मुझे आशा हैं कि उन्हें इस प्रबंध से कुछ विचार सामग्री मिलेगी। इस विषय के व्यावहारिक महत्त्व के साथ ही जाति प्रथा एक सर्वव्यापी व्यवस्था है और इसका सैद्धांतिक आधार जानने की उत्कंठा मुझ में जगी। उसी के परिणामस्वरूप मैंने अपने विचार आप लोगों के सम्मुख उपस्थित किए, जिन्हें मैं सार्थक मानता हूं और वे बातें आपके समक्ष रखीं, जिन पर यह व्यवस्था टिकी है। मैं इतना हठधर्मी भी नहीं हूं कि यह सोच लूं कि मेरा कथन ब्रह्म वाक्य है या इस विचार-विमर्श में योगदान से बढ़कर कुछ है। मैं सोचता हूं कि धारा का प्रवाह गलत दिशा में मोड़ दिया गया है और इस आलेख का प्राथमिक उद्देश्य यह बताना है कि अनुसंधान का सही मार्ग कौन सा है, ताकि एक सत्य उजागर हो। हमें इस विषय के विश्लेषण में पक्षपात रहित रहना है। भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बल्कि इस विषय पर वैज्ञानिक और निष्पक्ष रूप से विचार किया जाए। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि मेरा दृष्टिकोण सही दिशा में है, मुद्दे पर जो असहमति है, वह तार्किक है, फिर भी कुछ बातों पर सदा असहमति बनी रह सकती है, अंत में मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने जातिप्रथा के बारे में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यदि यह आधारहीन लगेगा तो मैं इसे तिलांजलि दे दूंगा।
Click Here For Read In English